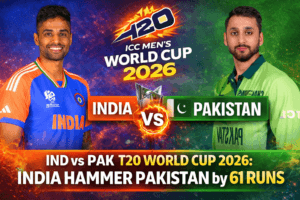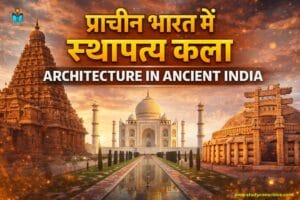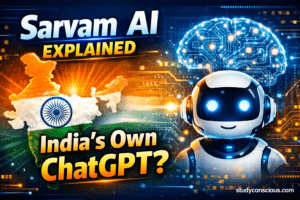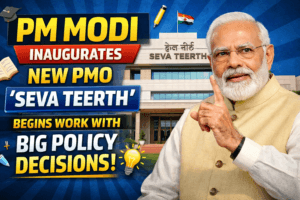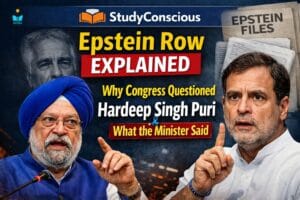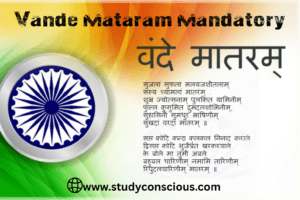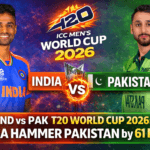मृदा, जिसे मिट्टी भी कहा जाता है, पृथ्वी की सतह की वह ऊपरी परत है जिसमें खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, पानी, वायु और जीवित जीवों का मिश्रण होता है। यह परत पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करती है और विभिन्न जीवों का आवास भी होती है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों में चट्टानों के टूटने, जैविक पदार्थों के विघटन और अन्य भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है।

मृदा के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
- खनिज कण: इसमें रेत, सिल्ट और मिट्टी शामिल हैं। ये कण मृदा की बनावट और जलधारण क्षमता को निर्धारित करते हैं।
- जैविक पदार्थ: इसमें पत्तियाँ, जड़ें, सूक्ष्मजीव और मृत जीव शामिल होते हैं जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं।
- जल: यह पौधों को आवश्यक नमी और पोषक तत्व प्रदान करता है।
- वायु: मृदा में ऑक्सीजन और अन्य गैसों का संतुलन पौधों की जड़ों और जीवाणुओं के लिए आवश्यक होता है।
- जीवित जीव: इसमें कीट, कृमि, सूक्ष्मजीव आदि शामिल हैं जो मृदा की संरचना और उपजाऊता को प्रभावित करते हैं।
मृदा का महत्व:
- कृषि: मृदा का प्रमुख उपयोग कृषि में होता है, जहां यह फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है।
- वनस्पति आवरण: यह पेड़-पौधों और अन्य वनस्पतियों के लिए आधार प्रदान करती है।
- पर्यावरण संतुलन: मृदा जलवायु, जल चक्र और जैव विविधता को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारत की मृदाओं का वर्गाीकरण
1. जलोढ़ मिट्टी:
* यह सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है, जो नदियों द्वारा जमा की गई गाद से बनती है। * यह उत्तरी भारत के गंगा-ब्रह्मपुत्र-सिंधु नदी घाटियों में पाए जाते हैं। * यह मिट्टी उपजाऊ, कई पोषक तत्वों से भरपूर और कई प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
2. काली मिट्टी:
* इसे डेक्कन ब्लैक मिट्टी भी कहा जाता है। * यह ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। * यह मिट्टी गहरी, काली, चिकनी और उच्च जल धारण क्षमता वाली होती है। * यह कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
3. लाल मिट्टी:
* यह प्रायद्वीपीय भारत में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। * यह प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से बनती है। * यह मिट्टी कम उपजाऊ, रेतीली और लाल रंग की होती है। * यह चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और अन्य दलहनों के लिए उपयुक्त होती है।
4. लैटेराइट मिट्टी:
* यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। * यह भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण चट्टानों के अपक्षय से बनती है। * यह मिट्टी कम उपजाऊ, अम्लीय और लाल-भूरे रंग की होती है। * यह चाय, कॉफी, रबर और नारियल जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
5. वन और पर्वतीय मिट्टी:
* यह हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। * यह जैविक पदार्थों के अपघटन से बनती है। * यह मिट्टी पतली, अम्लीय और कम उपजाऊ होती है। * यह फलों, सब्जियों और वनस्पतियों के लिए उपयुक्त होती है।
6. शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी:
* यह राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। * यह रेत और सिल्ट से भरपूर होती है। * यह मिट्टी कम उपजाऊ और नमक से भरपूर होती है। * यह बाजरा, गेहूं और ज्वार जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
7. लवणीय और क्षारीय मिट्टी:
* यह तटीय क्षेत्रों और अंतर्देशीय नमकीन क्षेत्रों में पाई जाती है। * यह मिट्टी उच्च मात्रा में नमक और क्षार से युक्त होती है। * यह अधिकांश फसलों के लिए अनुपयुक्त होती है। * कुछ विशेष फसलें, जैसे धान और ज्वार
कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु
- मृदा शब्द की उत्पति, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है. फर्श
- भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ कछारी मृदा पायी जाती है।
- रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है।
- रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है।
- मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता होता है।
- काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
- मिट्टी का पीला रंग फेरिक आक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के आक्साईड के कारण होता है।
- लैटेराइट मृदा मुख्यतः केरल,कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों में पाया जाता है।
- लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण लैटेराइट मृदा दिनों-दिन अनुर्वर होती है।
- मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।
- लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है।
- सबसे कम जलधारण क्षमता बलुई दोमट मृदा में पाया जाता है।
- पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होता है।
- मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसल उगाई जाती है।
- चम्बल घाटी का निर्माण अवनालिका अपरदन से हुआ है।
- चाय बागानों के लिए लैटेराइट मृदा उपयुक्त है।
- दोमट मृदा में गाद,मृतिका, व रेत के कण पाये जाते है।
- भारत की मृदाओं में सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी जस्ता के कारण होता है।
- गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है।
- अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु लाइम या चूना खनिज का प्रयोग किया जाता है।
- भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उतर प्रदेश राज्य में पायी जाती है।
- लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पायी जाती है।
- जैव मृदा का रंग नीला अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है।
- पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पायी जाती है।
- मरूस्थलीय मृदा में पोषक नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है।
- मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है।
- लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। जिससे नाइट्रोजन फॉस्फोरस एवं हृाूमस की कमी होती है।
PH मान के अनुसार मृदा की प्रकृति
| PH मान | मिट्टी की प्रकृति |
| 1 से 6 | अम्लीय मिट्टी (Acidic Soil) |
| 7 | उदासीन मिट्टी (Neutral Soil) |
| 8 से 14 | क्षारीय मिट्टी (Alkaline Soil) |