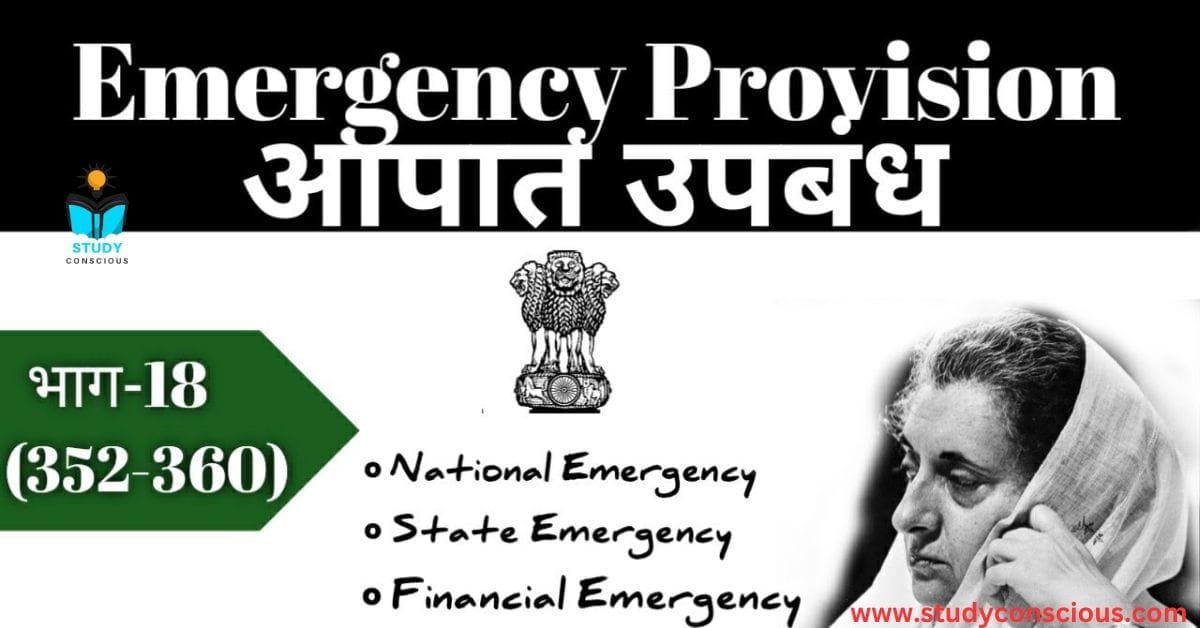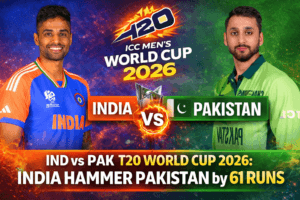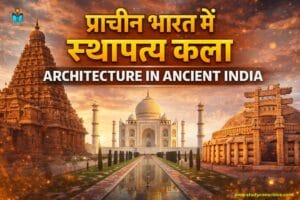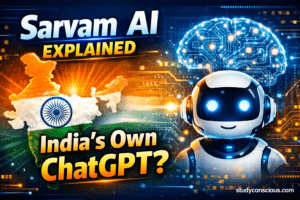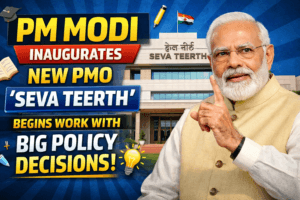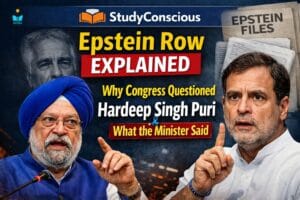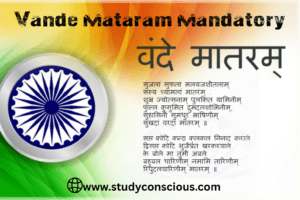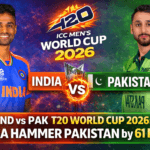आपात उपबंध (Emergency Provisions) भारत के संविधान में ऐसी प्रावधान हैं जो संकट की स्थितियों में केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। ये प्रावधान संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य देश की अखंडता, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना है।
आपात उपबंध के प्रकार
भारत के संविधान में तीन प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) – अनुच्छेद 352
यह तब लागू किया जाता है जब:
- देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से खतरा हो।
- इसे राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है।
- संसद को इसे 1 महीने के भीतर मंजूरी देनी होती है।
- प्रभाव:
- केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में दखल देने की शक्ति मिलती है।
- मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) निलंबित किए जा सकते हैं।
- वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार केंद्र के पास आ जाते हैं।
2. राज्य आपातकाल (President’s Rule) – अनुच्छेद 356
यह तब लागू किया जाता है जब:
- किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र (Constitutional Machinery) विफल हो जाए।
- राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।
- प्रभाव:
- राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है।
- राज्यपाल के माध्यम से राज्य का शासन केंद्र सरकार चलाती है।
- संसद राज्य के मामलों पर कानून बना सकती है।
3. आर्थिक आपातकाल (Financial Emergency) – अनुच्छेद 360
यह तब लागू किया जाता है जब:
- देश की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा हो।
- प्रभाव:
- राष्ट्रपति सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित कर सकते हैं।
- राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
- सरकारी कर्मचारियों की वेतन में कटौती की जा सकती है।
आपात उपबंध के कार्य:
- राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना: आपातकालीन परिस्थितियों में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं।
- राज्य सरकारों का नियंत्रण: राज्य आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी लेता है।
- आर्थिक स्थिरता बनाए रखना: आर्थिक आपातकाल वित्तीय संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है।
- मौलिक अधिकारों का निलंबन: यदि आवश्यक हो, तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं ताकि आपात स्थिति का समाधान हो सके।
- देश की संप्रभुता की रक्षा: बाहरी आक्रमण या युद्ध जैसी स्थितियों में केंद्र सरकार को प्रभावी उपाय करने का अधिकार दिया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में तीन बार लागू हुआ है:
- 1962 (चीन युद्ध)
- 1971 (पाकिस्तान युद्ध)
- 1975-77 (आंतरिक आपातकाल)।
- राज्य आपातकाल कई बार लागू हो चुका है।
- आर्थिक आपातकाल आज तक कभी लागू नहीं हुआ है।
आपात उपबंध का मुख्य उद्देश्य देश को किसी भी संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करना है, लेकिन इनका दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है।
अब तक की गई आपात उदघोषणाएँ –
भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा की गई है। ये आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किए गए थे। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:
1. 1962 का आपातकाल (चीन-भारत युद्ध के दौरान)
घोषणा की तारीख: 26 अक्टूबर 1962
कारण: चीन के साथ युद्ध।
विवरण:
भारत-चीन युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा को खतरा होने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। यह आपातकाल युद्ध की समाप्ति के बाद भी 1968 तक लागू रहा। यह भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल था।
2. 1971 का आपातकाल (पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान)
घोषणा की तारीख: 3 दिसंबर 1971
कारण: भारत-पाकिस्तान युद्ध।
विवरण:
इस युद्ध का परिणाम बांग्लादेश के निर्माण के रूप में हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने के कारण यह आपातकाल घोषित किया गया। यह आपातकाल 1977 तक लागू रहा क्योंकि इसे अगले आपातकाल (1975) से जोड़ा गया था।
3. 1975 का आपातकाल (आंतरिक अशांति के कारण)
घोषणा की तारीख: 25 जून 1975
कारण: आंतरिक अस्थिरता।
विवरण:
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह आपातकाल घोषित किया। इसमें प्रेस पर सेंसरशिप, नागरिक अधिकारों का निलंबन, और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। यह आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे विवादास्पद घटना माना जाता है। इसे 21 मार्च 1977 को समाप्त किया गया।
आपात उपबंध के मुख्य बिंदु:
- आपातकाल मे संसद के द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- हदय कुँजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।
- राज्य मे राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर राष्टपति लागू किया जाता है।
- राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक कि अवधि तक लगाया जा सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्व आक्रमण अथवा सशस़्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहा आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यो की रक्षा करें।
- भारतीय संविधान के 356 अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
- भारत मं वितिय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है।
- राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत स्थगित कर सकता है।
- संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह की अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लागू किया गया था।
- राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढाई जा सकती है, लेकिन एक बार मे ंकेवल एक वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है।
- मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्ािान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था।