राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग अपने देश के प्रति गहन प्रेम और निष्ठा व्यक्त करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रबल रूप से प्रभावित किया

राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व
- सांस्कृतिक जागरूकता: भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रमुख तत्व भारतीय संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के प्रति गर्व था। समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।
- राजनीतिक चेतना: 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- स्वराज की मांग: प्रारंभ में सुधार की मांग करने वाले नेताओं से आगे बढ़कर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने स्वराज (स्व-शासन) की मांग की।
प्रमुख घटनाएँ और आंदोलन
- 1857 का विद्रोह: इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को उजागर किया।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने भारतीयों को एक मंच प्रदान किया, जहां से वे अपनी मांगें और असंतोष व्यक्त कर सकते थे।
- असहयोग आंदोलन (1920-22): महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया। लोगों ने ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा।
- नमक सत्याग्रह (1930): दांडी मार्च के माध्यम से गांधीजी ने ब्रिटिश नमक कानून का विरोध किया और स्वराज की मांग को और मजबूती दी।
- भारत छोड़ो आंदोलन (1942): द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम और निर्णायक मांग के रूप में उभरा।
प्रारंभिक चरण
- प्रारंभिक प्रतिरोध: 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ ही भारतीयों के बीच असंतोष बढ़ने लगा। 1857 का सिपाही विद्रोह (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम) राष्ट्रवाद का पहला व्यापक प्रयास माना जा सकता है, यद्यपि यह सफल नहीं हुआ।
- सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन: राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, और अन्य समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाई और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पुनरुद्धार किया। इसने भारतीयों में आत्म-सम्मान और राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत किया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885): 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने राष्ट्रवाद को एक संगठित रूप दिया। कांग्रेस के शुरुआती नेता नरमपंथी थे, जो ब्रिटिश शासन में सुधार के पक्षधर थे। इनमें दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रमुख थे।
20वीं शताब्दी और गांधी युग
- चरमपंथी राष्ट्रवाद: 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने नरमपंथियों के बजाय उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाया और स्वराज (स्व-शासन) की मांग की।
- महात्मा गांधी का आगमन: 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद, राष्ट्रवाद को एक नया आयाम मिला। गांधीजी ने सत्याग्रह, अहिंसा, और असहयोग आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन चलाए।
- असहयोग आंदोलन (1920-22): इस आंदोलन के तहत गांधीजी ने लोगों से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने का आह्वान किया।
- नमक सत्याग्रह (1930): दांडी मार्च के माध्यम से गांधीजी ने नमक पर ब्रिटिश कर के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध किया।
- भारत छोड़ो आंदोलन (1942): द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम मांग के रूप में उभरा।
मुस्लिम लीग और विभाजन
- मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग: 20वीं शताब्दी के मध्य में, मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की। इसके परिणामस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
स्वतंत्रता प्राप्ति
- स्वतंत्रता और विभाजन (1947): 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। विभाजन के दौरान भारी हिंसा और जनसंख्या का आदान-प्रदान हुआ।
निष्कर्ष
भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक सतत प्रक्रिया थी जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, और राजनीतिक तत्व शामिल थे। इसने भारतीय समाज को एकजुट किया और अंततः स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी न केवल संघर्ष की है बल्कि आत्म-सम्मान, स्वाधीनता और मानव अधिकारों की पुनर्प्राप्ति की भी है।





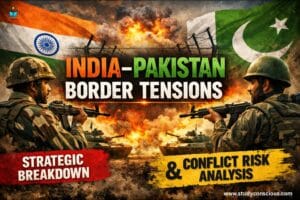


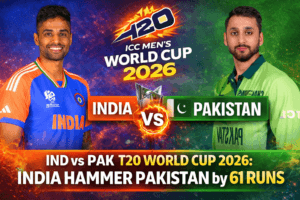



Awesome