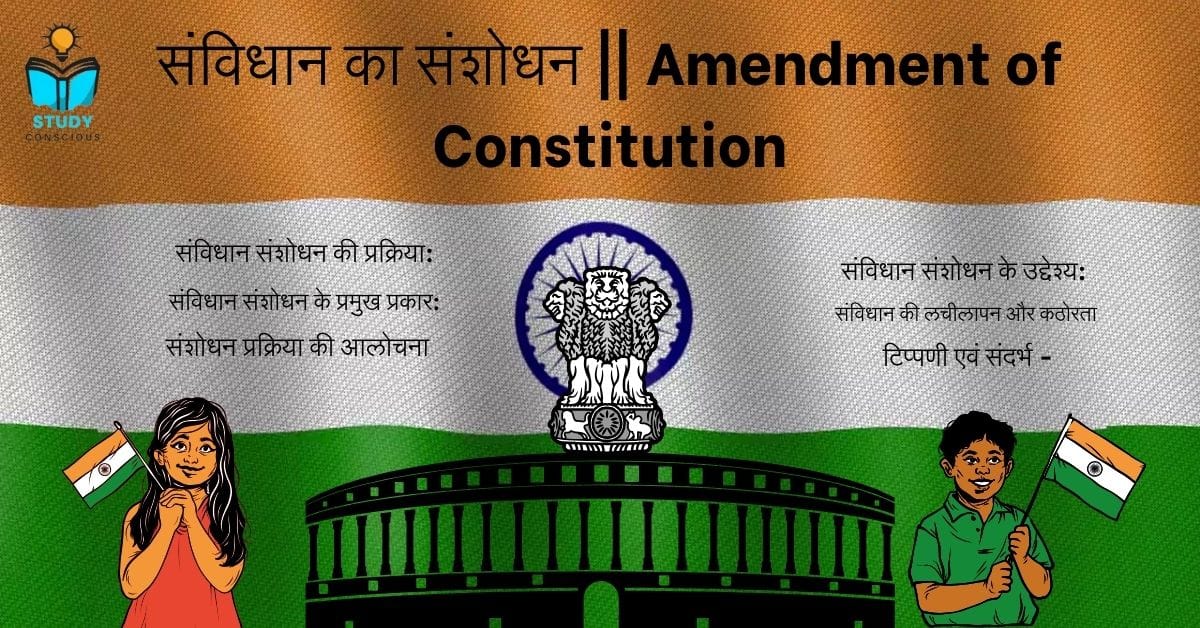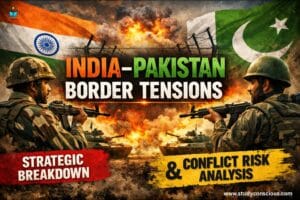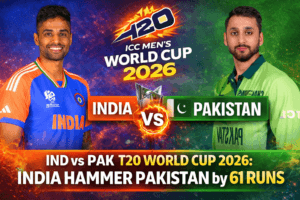भारतीय संविधान के संशोधन का तात्पर्य संविधान में परिवर्तन, सुधार, या वृद्धि करने की प्रक्रिया से है। भारतीय संविधान को संशोधित करने का प्रावधान संविधान के भाग XX के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, संसद को संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया:
- प्रस्तावना:
- संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है।
- प्रस्ताव को पेश करने के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है।
- मंजूरी:
- संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव को दोनों सदनों में अलग-अलग, कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति:
- दोनों सदनों से पारित होने के बाद, प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही संविधान संशोधन अधिनियम बनता है और लागू होता है।
- राज्यों की स्वीकृति (विशेष मामलों में):
- कुछ संशोधन, जैसे कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित, या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामलों में, संसद की मंजूरी के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी स्वीकृति आवश्यक होती है।
संविधान संशोधन के प्रमुख प्रकार:
- सरल बहुमत से संशोधन:
- कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के केवल सरल बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे कि अनुसूचियों में परिवर्तन।
- विशेष बहुमत से संशोधन:
- अधिकांश संशोधनों के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
- विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से संशोधन:
- महत्वपूर्ण प्रावधानों को संशोधित करने के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है।
संविधान संशोधन के उद्देश्य:
- प्रगति और परिवर्तनशीलता:
- समय के साथ आवश्यक सुधार और परिवर्तन करना।
- सामाजिक और आर्थिक सुधार:
- समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना।
- संवैधानिक विवादों का समाधान:
- संविधान के प्रावधानों में स्पष्टता लाना और विवादों का समाधान करना।
संविधान संशोधन के उदाहरण:
- पहला संशोधन (1951): भूमि सुधार कानूनों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए।
- 42वां संशोधन (1976): संविधान को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- 73वां और 74वां संशोधन (1992): पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए।
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है:
1. संशोधन प्रस्ताव की प्रस्तुति
- संसद के किसी भी सदन में: संशोधन प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसे संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
- अधिसूचना: सदन के सचिवालय में इस प्रस्ताव को उचित नोटिस के साथ जमा करना होता है।
2. बहस और मतदान
- पहला पाठन: प्रस्ताव पेश करने के बाद, इसे सदन के सदस्यों के बीच बहस के लिए रखा जाता है।
- मतदान: संशोधन प्रस्ताव को पारित करने के लिए, प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो तिहाई बहुमत आवश्यक है।
- विशेष बहुमत: कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।
3. राज्यों की स्वीकृति (विशेष मामलों में)
कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनके लिए राज्यों की विधानसभाओं की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। ये संशोधन निम्नलिखित मामलों से संबंधित होते हैं:
- संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित।
- न्यायपालिका की संरचना और शक्तियों से संबंधित।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित।
- राज्यसभा और विधान परिषदों के गठन और संरचना से संबंधित।
इस प्रकार के संशोधनों के लिए, संसद में पारित होने के बाद, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक है।
4. राष्ट्रपति की स्वीकृति
- संविधान संशोधन अधिनियम: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने पर, प्रस्ताव संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है और लागू होता है।
5. अधिनियम का प्रवर्तन
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, संशोधन अधिनियम राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित होता है और उसे संविधान में शामिल किया जाता है। इस प्रकार संशोधन प्रभावी हो जाता है।
विशेष प्रकार के संशोधन
- सरल बहुमत से संशोधन:
- कुछ मामलों में, जैसे कि संसद के नियम और कार्यविधि में परिवर्तन, संसद के केवल सरल बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है।
- विशेष बहुमत से संशोधन:
- अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
- विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति:
- संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए, संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है।
साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जाने वाले प्रावधान
- संसद की नियमावली:
- संसद के सदनों की नियमावली और कार्यविधि में बदलाव।
- लोकसभा और राज्यसभा की संचालन प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में परिवर्तन।
- राज्य पुनर्गठन:
- राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन, नए राज्यों का निर्माण, और पुराने राज्यों का विभाजन।
- इस प्रकार के संशोधनों को संविधान (अनुच्छेद 2 और 3) के तहत साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है।
- अनुसूचियों में परिवर्तन:
- संविधान की अनुसूचियों (Schedules) में परिवर्तन या संशोधन।
- उदाहरण: अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन।
- कुछ वित्तीय मामलों में:
- राज्यसभा में धन विधेयक (Money Bill) को पारित करने की प्रक्रिया।
- वार्षिक बजट और संबंधित वित्तीय विधेयक भी साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं।
- अन्य गैर-मौलिक प्रावधान:
- कुछ गैर-मौलिक प्रावधानों में संशोधन या उन्हें निरस्त करना, जो संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) को प्रभावित नहीं करते हैं।
साधारण बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया
- प्रस्तावना:
- संसद के किसी भी सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित होने वाले प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है।
- सदन के सचिवालय में उचित नोटिस के साथ प्रस्ताव जमा करना होता है।
- बहस और मतदान:
- प्रस्ताव पेश होने के बाद, सदन में इस पर बहस होती है।
- बहस के बाद, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति:
- संसद में पारित होने के बाद, प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर, प्रस्ताव लागू हो जाता है और संविधान में संशोधन के रूप में शामिल किया जाता है
संशोधन प्रक्रिया की आलोचना
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को कई दृष्टिकोणों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम समझ सकते हैं कि आलोचना के मुख्य पहलू क्या हैं:
1. संविधान की लचीलापन और कठोरता
- लचीलापन: कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान में बदलाव करना बहुत आसान है। संसद में साधारण बहुमत से किए जाने वाले संशोधनों के कारण, सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में बदलाव कर सकती हैं।
- कठोरता: दूसरी ओर, कुछ लोग इसे अत्यधिक कठोर मानते हैं, खासकर महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिससे आवश्यक सुधारों को लागू करना मुश्किल हो सकता है।
2. राजनीतिक दुरुपयोग
- सत्तारूढ़ पार्टी का प्रभुत्व: यह देखा गया है कि कई बार सत्तारूढ़ पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए संविधान संशोधनों का उपयोग करती है। इससे संविधान की मूल भावना को खतरा हो सकता है।
- आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति: कई बार संशोधन आर्थिक और सामाजिक सुधारों के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए किए जाते हैं, जिससे संविधान की संरचना और उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
3. संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन
- मूल ढांचा सिद्धांत: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदले जाने का सिद्धांत स्थापित किया। हालांकि, कई बार ऐसे संशोधन प्रस्तावित होते हैं जो इस सिद्धांत का उल्लंघन कर सकते हैं।
- न्यायिक हस्तक्षेप: कई बार न्यायालय को संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के लिए संशोधनों को रद्द करना पड़ता है, जिससे न्यायपालिका और विधायिका के बीच तनाव बढ़ता है।
4. राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता
- संघीय ढांचा: संघीय ढांचे से संबंधित संशोधनों के लिए राज्यों की मंजूरी आवश्यक है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और समय लेने वाली है, जिससे आवश्यक सुधारों को लागू करना कठिन हो जाता है।
- क्षेत्रीय असंतुलन: राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता के कारण कभी-कभी क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे कुछ राज्यों की अनदेखी हो सकती है।
5. साधारण बहुमत से संशोधन
- महत्वपूर्ण प्रावधानों का संशोधन: साधारण बहुमत से कुछ प्रावधानों का संशोधन करना आसान हो सकता है, लेकिन यह संविधान की स्थिरता और अखंडता को खतरे में डाल सकता है।
- संविधान का सम्मान: साधारण बहुमत से किए गए संशोधन कई बार संविधान की पवित्रता और महत्व को कम कर सकते हैं।
6. जन भागीदारी का अभाव
- जनता की भागीदारी: संशोधन प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी का अभाव है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन संविधान संशोधन के मामलों में यह सीमित रहती है।
- जनमत संग्रह: कई लोकतांत्रिक देशों में महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के लिए जनमत संग्रह (Referendum) का प्रावधान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में लचीलापन और कठोरता का संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत, और जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पुनर्विचार और सुधार की आवश्यकता है। आलोचनाओं के बावजूद, यह प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की प्रासंगिकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
टिप्पणी एवं संदर्भ –
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973
- 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया।
- सुभाष सी कश्यप, अवर पार्लियामेंट, नेशनल बुक ट्रस्ट 1999 पृष्ठ- 168
- इस प्रावधान को 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 279-ए से संबंधित है।
- अमेरिका में भी कांग्रेस (अमेरिकी विधायिका) द्वारा दो-तिहाई राज्य विधानमण्डलों की याचिका संविधानिक सभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है।।
- के सी व्हेयर, मॉडर्न कांस्टीट्यूशंस, 1966.
- कांस्टीट्सूएंट असेंबली डिबेट्स
- ग्रीनविल ऑस्टिन, द इंडियन कांस्टीट्यूशन: कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन ऑक्सफोर्ड 1966