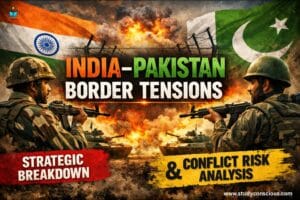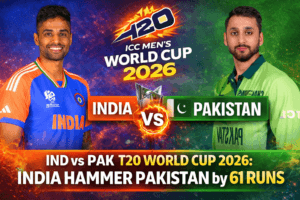भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक, उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता न्यायक्षेत्र शक्तियां प्रक्रिया आदि का उल्लेख हैं। संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है।
भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया । यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उतराधिकारी था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्यायक्षेत्र पूर्ववर्ती से ज्यदा व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वाेच्च न्यायालय था।
संरचना और नियुक्ति
संरचना:
उच्चतम न्यायालय की संरचना में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:
- मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI):
- उच्चतम न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता है।
- वह अदालत के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों की देखरेख करता है।
- अन्य न्यायाधीश (Puisne Judges):
- उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं।
- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।
नियुक्ति:
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- परंपरा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति:
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर करते हैं।
- कोलेजियम प्रणाली (Collegium System):
- न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कोलेजियम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
- कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- यह प्रणाली नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
- योग्यता:
- उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
- वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या
- उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्षों तक वकील रहा हो या
- राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट न्यायविद (distinguished jurist) हो।
- उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
- कार्यकाल:
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं।
- न्यायाधीश स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले सकते हैं या राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग (impeachment) के माध्यम से हटाए जा सकते हैं यदि वे संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत कदाचार (misbehavior) या अक्षमता (incapacity) के आधार पर दोषी पाए जाते हैं।
अर्हताएं, शपथ और वेतन
अर्हताएं (Qualifications):
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं:
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश:
- वह व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो।
- वकील:
- वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्षों तक वकील रहा हो।
- विशिष्ट न्यायविद (Distinguished Jurist):
- राष्ट्रपति की राय में वह व्यक्ति एक विशिष्ट न्यायविद (jurist) होना चाहिए।
शपथ (Oath):
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची (Third Schedule) में निर्दिष्ट है। शपथ में न्यायाधीश निम्नलिखित प्रतिज्ञा करते हैं:
- वे भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे।
- वे भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे।
- वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी डर या पक्षपात के करेंगे।
- वे संविधान और कानूनों के अनुसार न्याय करेंगे।
वेतन (Salary):
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और अन्य भत्तों का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में:
- मुख्य न्यायाधीश का वेतन:
- मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 रुपये है।
- अन्य न्यायाधीशों का वेतन:
- अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपये है।
अन्य भत्ते और सुविधाएं:
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं और भत्ते भी प्राप्त होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- आवास:
- न्यायाधीशों को सरकारी आवास की सुविधा प्रदान की जाती है।
- चिकित्सा सुविधाएं:
- न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
- भत्ता:
- न्यायाधीशों को कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, जैसे कि यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता, आदि।
- पेंशन:
- सेवा निवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं
कार्यकाल और निष्कासन
कार्यकाल (Tenure):
- सेवानिवृत्ति की आयु:
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यह संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत निर्धारित है।
- स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति:
- न्यायाधीश अपनी इच्छा से निर्धारित उम्र से पहले भी सेवानिवृत्ति ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचित करना होता है।
निष्कासन (Removal):
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए एक कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायिक सेवा (महाभियोग) अधिनियम, 1968 के तहत निर्धारित है।
- महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया:
- न्यायाधीश को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है।
- महाभियोग के लिए निम्नलिखित आधार हो सकते हैं:
- कदाचार (Misbehavior)
- अक्षमता (Incapacity)
- महाभियोग प्रस्ताव:
- महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।
- जाँच समिति (Inquiry Committee):
- महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद एक तीन-सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें:
- उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश
- एक विशिष्ट विधिवेत्ता (eminent jurist)
- यह समिति आरोपों की जाँच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है।
- महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद एक तीन-सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें:
- संसदीय मतदान:
- अगर जाँच समिति न्यायाधीश के खिलाफ आरोप सही पाती है, तो संसद में मतदान होता है।
- प्रस्ताव को पास करने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से समर्थन आवश्यक है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति:
- दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके बाद न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है।
कार्यकारी, तदर्थ और सेवानिवृति न्यायाधीश
1. कार्यकारी न्यायाधीश (Acting Judges):
उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालयों में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 224(2) के तहत है। कार्यकारी न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाते हैं जब:
- न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं होती।
- किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर अदालत का कामकाज प्रभावित हो रहा हो।
2. तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judges):
उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत की जा सकती है। यह तब किया जाता है जब:
- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की आवश्यक संख्या उपलब्ध नहीं होती।
- मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श के बाद इस बात की राय व्यक्त करते हैं कि अदालत के कामकाज के लिए तदर्थ न्यायाधीश की आवश्यकता है।
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया:
- मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा करते हैं।
- उच्च न्यायालय के संबंधित मुख्य न्यायाधीश और संबंधित न्यायाधीश की सहमति के बाद यह नियुक्ति की जाती है।
3. सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judges):
संविधान के अनुच्छेद 128 के तहत, उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी आधार पर काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है:
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह मानता है कि अदालत के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की आवश्यकता है।
- ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उस न्यायाधीश की सहमति आवश्यक होती है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भूमिका:
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में अस्थायी रूप से काम करने के लिए बुलाया जा सकता है।
- उनकी स्थिति, अधिकार, और विशेषाधिकार वैसे ही होते हैं जैसे वर्तमान न्यायाधीशों के होते हैं, लेकिन वे पेंशन के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अर्जित लाभों के पात्र रहते हैं।
सारांश:
- कार्यकारी न्यायाधीश: यह प्रावधान उच्च न्यायालयों के लिए होता है, जब अस्थायी रूप से अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।
- तदर्थ न्यायाधीश: उच्चतम न्यायालय में अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर पूर्व न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति।
उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता
उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता (Independence of the Supreme Court)
उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता भारत की न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न्यायिक प्रणाली को निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान और तंत्र स्थापित किए गए हैं:
1. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions):
- संविधान के अनुच्छेद 50: यह अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण का प्रावधान करता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
- अनुच्छेद 124 से 147: ये अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, और अन्य प्रावधानों को निर्धारित करते हैं, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं।
2. न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges):
- कोलेजियम प्रणाली (Collegium System): न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कम करने के लिए कोलेजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
3. न्यायाधीशों का कार्यकाल और निष्कासन (Tenure and Removal of Judges):
- नियत कार्यकाल: न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जिससे उनके निर्णयों पर किसी बाहरी दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता।
- महाभियोग (Impeachment): न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर और जटिल होती है, जिससे उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया न्यायाधीशों को निष्पक्ष और निर्भीक होकर कार्य करने में सहायक होती है।
4. वेतन और भत्ते (Salary and Allowances):
- न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, और इन्हें कार्यपालिका के विवेक पर नहीं छोड़ा जाता। वेतन और भत्ते की यह स्थिरता न्यायाधीशों की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
5. स्वतंत्रता की सुरक्षा (Security of Tenure):
- न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन में सुरक्षा और स्थिरता उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है।
6. न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review):
- उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, जिससे वह संविधान के विपरीत किसी भी कानून या आदेश को निरस्त कर सकता है। यह कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होता है।
7. न्यायिक आचरण संहिता (Code of Conduct for Judges):
- न्यायाधीशों के लिए एक आचरण संहिता निर्धारित है, जिससे वे नैतिक और पेशेवर मानकों का पालन करते हैं और किसी भी प्रकार की पक्षपात या भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं।
8. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression):
- न्यायाधीशों को उनके विचारों और निर्णयों में स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्हें न्यायिक मामलों में स्वतंत्रता से निर्णय लेने की अनुमति है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के।
9. स्वतंत्र न्यायालय परिसर (Independent Court Complex):
- न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों के काम करने के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है, जिससे वे बिना किसी दबाव के अपने निर्णय ले सकें।
उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार
उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार (Powers and Jurisdiction of the Supreme Court of India)
उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा विविध प्रकार की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। यह न केवल एक सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, बल्कि भारतीय न्यायिक प्रणाली का संरक्षक भी है।
1. मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction):
- संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत, उच्चतम न्यायालय के पास संघ और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच विवादों का निपटान करने का अधिकार है। यह क्षेत्राधिकार विशेष रूप से संघीय विवादों के लिए होता है।
- संवैधानिक विवाद: संघ और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवाद भी उच्चतम न्यायालय में सीधे लाए जा सकते हैं।
2. अपील क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction):
- नागरिक और आपराधिक मामलों में अपील: उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133, और 134 के तहत यह अधिकार निर्दिष्ट है।
- संवैधानिक मामलों में अपील: संविधान के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
3. सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction):
- संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी संवैधानिक या विधिक प्रश्न पर सलाह मांग सकते हैं। यह सलाह अनिवार्य नहीं होती, लेकिन इसका महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रभाव होता है।
4. विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition – SLP):
- संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत, उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है। यह अपील का एक असाधारण उपाय है और उच्चतम न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है।
5. संवैधानिक व्याख्या (Interpretation of Constitution):
- उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करने और संवैधानिक प्रश्नों का निर्णय करने का अंतिम प्राधिकरण है। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत आती है, जो न्यायालय के निर्णयों को सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी बनाती है।
6. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (Protection of Fundamental Rights):
- संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति है जैसे कि हाबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, और सेर्टिओरारी।
7. न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review):
- उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, जिसके तहत वह संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जाँच कर सकता है और उन्हें असंवैधानिक पाए जाने पर निरस्त कर सकता है।
8. स्वतंत्रता और निष्पक्षता:
- उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और निष्कासन से जुड़े प्रावधान बनाए गए हैं। न्यायालय की स्वायत्तता न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखती है।
सारांश:
उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार निम्नलिखित बिंदुओं में समाहित होते हैं:
- मूल क्षेत्राधिकार: संघ और राज्यों के बीच विवाद।
- अपील क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील।
- सलाहकार क्षेत्राधिकार: राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह।
- विशेष अनुमति याचिका: असाधारण मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप।
- संवैधानिक व्याख्या: संविधान की अंतिम व्याख्या।
- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा: मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करना।
- न्यायिक पुनरीक्षण: कानूनों की संवैधानिकता की जाँच।
उच्चतम न्यायालय की यह विस्तृत शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायिक प्रणाली की मजबूती और न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, जिससे न्याय की निष्पक्ष और स्वतंत्र वितरण संभव हो पाता है।
उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता
उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता (Advocates of the Supreme Court)
उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए अधिवक्ताओं को विशेष योग्यताओं और नियमों का पालन करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड, वरिष्ठ अधिवक्ता, और अन्य अधिवक्ता शामिल हैं।
1. अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड (Advocate-on-Record):
- योग्यता और परीक्षा: एक अधिवक्ता को अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड बनने के लिए उच्चतम न्यायालय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। यह परीक्षा चार साल तक उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने के बाद दी जा सकती है।
- विशेषाधिकार: अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का विशेषाधिकार होता है। यह जिम्मेदारी केवल अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के पास होती है और वे अन्य अधिवक्ताओं की ओर से भी याचिका दाखिल कर सकते हैं।
2. वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate):
- मनोनयन: वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता को प्रदान किया जाता है। यह दर्जा उन अधिवक्ताओं को दिया जाता है जो कानूनी ज्ञान, अनुभव और योगदान के मामले में उच्च मानकों को पूरा करते हैं।
- प्रतिबंध: वरिष्ठ अधिवक्ता खुद से याचिका दाखिल नहीं कर सकते और न ही वे सीधे किसी मामले का संचालन कर सकते हैं। उन्हें अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड या अन्य अधिवक्ताओं की सहायता लेनी होती है।
3. अन्य अधिवक्ता (Other Advocates):
- प्रैक्टिस: अन्य अधिवक्ता जो अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड नहीं हैं, वे भी उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वे सीधे याचिका दाखिल नहीं कर सकते। उन्हें किसी अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के माध्यम से याचिका दाखिल करनी होती है।
- प्रक्रियात्मक समर्थन: वे मामलों की सुनवाई में सहायता कर सकते हैं, और अदालत में दलीलें पेश कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा पूरी की जाती हैं।
4. अनुशासन और आचार संहिता (Discipline and Code of Conduct):
- नैतिकता और आचरण: उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को उच्च नैतिक मानकों और आचार संहिता का पालन करना होता है। इसका उल्लंघन करने पर उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया: सभी अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिनियम और नियमों का पालन करना होता है, जो अधिवक्ताओं की योग्यता, पंजीकरण और आचरण को नियंत्रित करते हैं।
सारांश:
- अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड: विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करके, याचिका दाखिल करने का विशेषाधिकार।
- वरिष्ठ अधिवक्ता: उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा विशेष दर्जा प्रदान, लेकिन याचिका सीधे दाखिल नहीं कर सकते।
- अन्य अधिवक्ता: उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन याचिका अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के माध्यम से दाखिल करनी होती है।
- आचार संहिता: उच्च नैतिक मानकों का पालन अनिवार्य, अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान।
उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं की यह श्रेणियाँ और उनके विशेषाधिकार अदालत के कार्य को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।
उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में
भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न पहलुओं, शक्तियों और कार्यों से संबंधित अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। इन अनुच्छेदों का संक्षेप में विवरण निम्नलिखित है:
1. अनुच्छेद 124:
- स्थापना और गठन: उच्चतम न्यायालय की स्थापना, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की संख्या।
2. अनुच्छेद 125:
- वेतन और भत्ते: मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों का निर्धारण।
3. अनुच्छेद 126:
- कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
4. अनुच्छेद 127:
- तदर्थ न्यायाधीश: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति।
5. अनुच्छेद 128:
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्चतम न्यायालय में अस्थायी तौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।
6. अनुच्छेद 129:
- अदालत का अभिधान: उच्चतम न्यायालय एक न्यायालय के रूप में कार्य करेगा और इसे रिकॉर्ड की अदालत माना जाएगा।
7. अनुच्छेद 130:
- सीट: उच्चतम न्यायालय की बैठकों का स्थान।
8. अनुच्छेद 131:
- मूल क्षेत्राधिकार: संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।
9. अनुच्छेद 132:
- अपील का क्षेत्राधिकार (संवैधानिक मामलों में): उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ संवैधानिक मामलों में अपील।
10. अनुच्छेद 133:
- नागरिक मामलों में अपील: उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ नागरिक मामलों में अपील।
11. अनुच्छेद 134:
- आपराधिक मामलों में अपील: उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ आपराधिक मामलों में अपील।
12. अनुच्छेद 134A:
- प्रमाण पत्र: अपील के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र देना।
13. अनुच्छेद 135:
- अधिकार का विस्तार: संसद द्वारा दी गई अतिरिक्त शक्तियों का उच्चतम न्यायालय पर लागू होना।
14. अनुच्छेद 136:
- विशेष अनुमति याचिका (SLP): न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका।
15. अनुच्छेद 137:
- पुनर्विचार: उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों का पुनर्विचार।
16. अनुच्छेद 138:
- अधिकार का विस्तार: संघ द्वारा किए गए समझौतों के आधार पर न्यायालय की शक्ति का विस्तार।
17. अनुच्छेद 139:
- रिट की शक्ति: उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति।
18. अनुच्छेद 140:
- सहायक शक्तियाँ: उच्चतम न्यायालय को सहायक शक्तियों का प्रावधान।
19. अनुच्छेद 141:
- न्यायिक मिसाल: उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे।
20. अनुच्छेद 142:
- पूर्ण न्याय करने की शक्ति: उच्चतम न्यायालय की निर्णय लेने की शक्ति।
21. अनुच्छेद 143:
- सलाहकार क्षेत्राधिकार: राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से विधिक प्रश्नों पर सलाह लेना।
22. अनुच्छेद 144:
- सहायता और अनुपालन: उच्चतम न्यायालय के आदेशों और निर्णयों का पालन सभी प्राधिकरणों द्वारा।
23. अनुच्छेद 145:
- नियम और प्रक्रिया: उच्चतम न्यायालय की कार्य प्रक्रिया और नियम।
24. अनुच्छेद 146:
- कर्मचारी और सेवाएँ: उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवाएँ।
25. अनुच्छेद 147:
- व्याख्या: संविधान के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या।
इन अनुच्छेदों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की संरचना, कार्यप्रणाली, शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है, जिससे भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और कार्यक्षमता सुनिश्चित होती है।