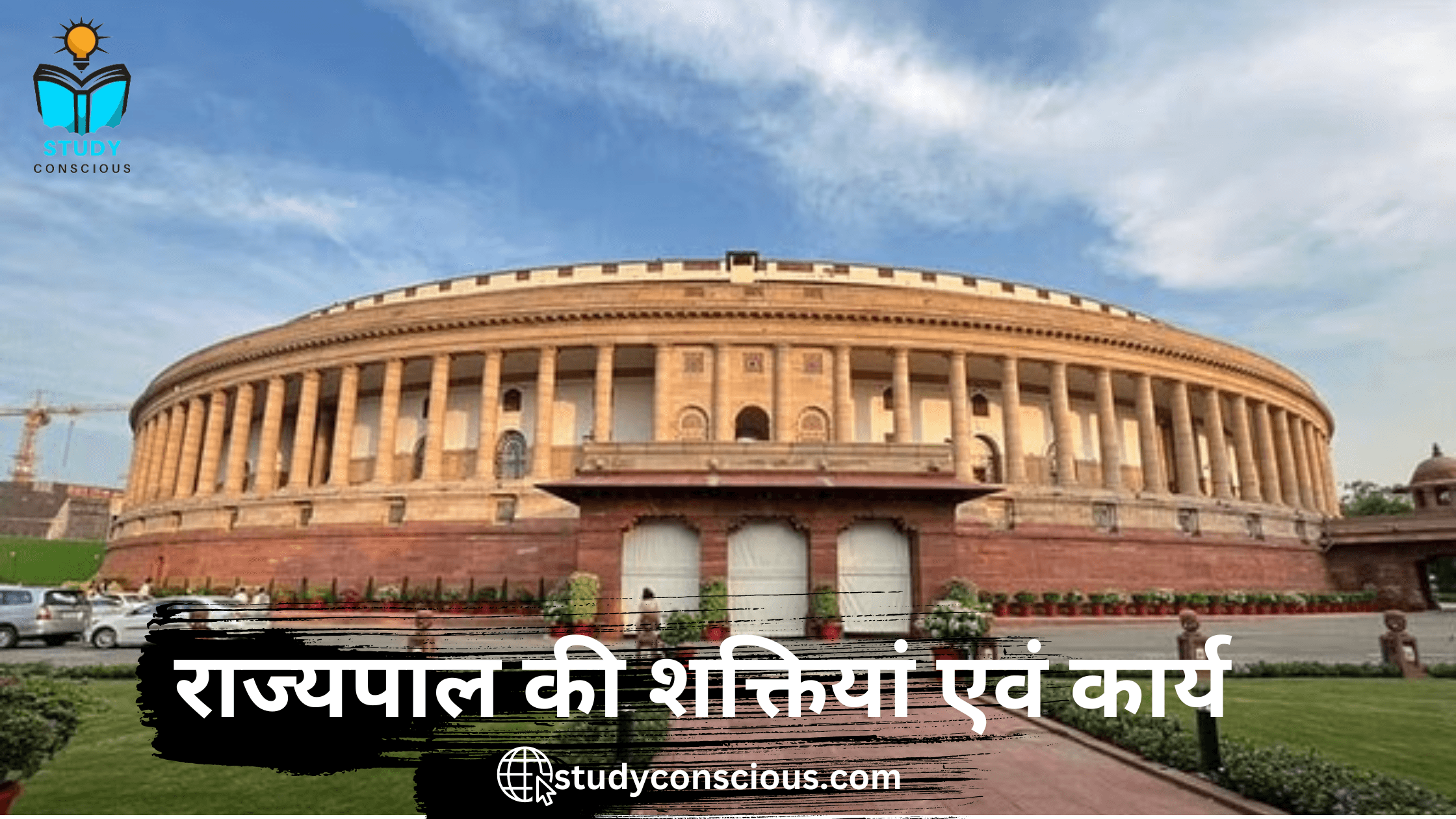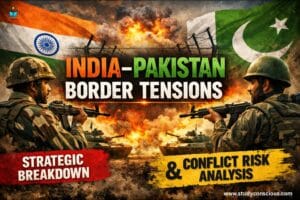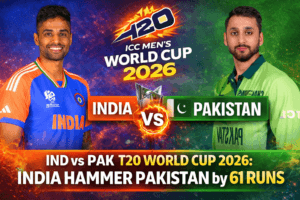भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है, जैसे कि केन्द्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य में सरकार के बारे मे बताया गया है।
संविधान के छठे भाग के अनुच्देद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे मंे बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते है – राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) इस तरह राज्य में उप-राज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता जैसे कि केद्र में उप-राट्रपति होते हैं।
राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक मुखिया) होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार कार्यालय, दोहरी भूमिका निभाता है।
सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकाता है।

राज्यपाल की नियुक्ति
भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पहले भी हटाए जा सकते हैं।
राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया:
- राष्ट्रपति का चयन: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें केंद्र सरकार की सलाह महत्वपूर्ण होती है।
- आवश्यक योग्यता: राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं:
- वह भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- उसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- कार्यकाल: राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति की सेवा में तब तक रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति उन्हें हटाने का निर्णय नहीं लेते।
- हटाने की प्रक्रिया: राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पष्ट कारण आवश्यक नहीं होता और न ही इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- शपथ ग्रहण: राज्यपाल की नियुक्ति के बाद, वह अपने पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है।
राज्यपाल की भूमिका और अधिकार विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि राज्य की विधायिका को बुलाना और भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना, और राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करना।
राज्यपाल के पद की शार्तें
राज्यपाल के पद के लिए भारतीय संविधान में कुछ विशेष शर्तें और योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ये शर्तें राज्यपाल के पद की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। निम्नलिखित शर्तें राज्यपाल के पद के लिए लागू होती हैं:
- नागरिकता: राज्यपाल को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आयु सीमा: राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभ के पद पर न होना: राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि वे किसी अन्य सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, जिसमें वेतन या अन्य लाभ मिलता हो।
- विधानमंडल का सदस्य न होना: राज्यपाल न तो संसद और न ही किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो पहले से किसी सदन का सदस्य है, राज्यपाल नियुक्त होता है, तो उसे अपने विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा।
- योग्यता: हालाँकि संविधान में कोई विशेष शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, परंतु राज्यपाल के पद के लिए सामान्यतः उन व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो उच्चतम स्तर पर प्रशासनिक अनुभव रखते हों या किसी महत्वपूर्ण पद पर रहे हों।
- पार्टी से निष्पक्षता: राज्यपाल को नियुक्ति के बाद राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें किसी राजनीतिक दल के प्रति वफादारी नहीं दिखानी चाहिए और राज्य के प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्ष रहना चाहिए।
ये शर्तें राज्यपाल के पद को गरिमामय बनाए रखने और उसके निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। राज्यपाल का मुख्य कार्य राज्य के संविधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना होता है और इस भूमिका में वे कई महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं
राज्यपाल की पदावधि
भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यपाल का कार्यकाल और पदावधि से संबंधित मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- कार्यकाल की अवधि: राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। यह कार्यकाल उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वे अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। हालांकि, यह अवधि पांच वर्षों की होती है, लेकिन वे राष्ट्रपति की सेवा में तब तक रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।
- हटाने का अधिकार: राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। इस संबंध में संविधान में कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है और राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- पुनः नियुक्ति: राज्यपाल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्हें फिर से उसी राज्य या किसी अन्य राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- स्थानांतरण: राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- कार्यकाल का विस्तार: यदि किसी कारणवश नए राज्यपाल की नियुक्ति में देरी होती है, तो वर्तमान राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति और शपथ ग्रहण नहीं हो जाती।
राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और उनके कार्यों में निष्पक्षता और गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण अपेक्षित है। राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और उनके कार्य राज्य की स्थिरता और संविधान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य
राज्यपाल भारतीय राज्यों में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है और उनकी शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं:
कार्यकारी शक्तियाँ:
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति: राज्यपाल चुनाव के बाद विधानमंडल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं।
- मंत्रिपरिषद की नियुक्ति: मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
- कार्यकारी आदेश: राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक मामलों को संचालित करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं।
- राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ: राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह कार्य वे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।
विधायी शक्तियाँ:
- विधानसभा के सत्र बुलाना और भंग करना: राज्यपाल विधानसभा के सत्रों को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
- विधेयकों को स्वीकृति: राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं या राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
- आवश्यक अध्यादेश जारी करना: जब विधानसभा सत्र में नहीं होती, तब राज्यपाल आवश्यक मामलों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो कि विधानमंडल द्वारा पारित कानून की तरह प्रभावी होते हैं।
न्यायिक शक्तियाँ:
- क्षमा प्रदान करना: राज्यपाल कुछ मामलों में दंड माफी, दंड कम करना, या दंड बदलने के लिए शक्ति रखते हैं।
- मृत्युदंड माफी: वे राज्य के न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड को माफ करने या उसे बदलने की शक्ति रखते हैं।
वित्तीय शक्तियाँ:
- वित्तीय विधेयक: कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- राज्य बजट: राज्य का वार्षिक बजट राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेष शक्तियाँ:
- विशेष जिम्मेदारी: राज्यपाल को संविधान द्वारा विशेष जिम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं, जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों की प्रशासनिक देखरेख।
- राष्ट्रपति शासन: यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
अनुच्छेद 356 के तहत:
राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य महत्वपूर्ण हैं और वे राज्य के सुचारू संचालन और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उनकी भूमिका का संतुलन और संवैधानिक प्रावधानों का पालन राज्य की स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करता है।
कार्यकारी शक्तियां
राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ राज्यपाल की प्रमुख कार्यकारी शक्तियों का विवरण दिया गया है:
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति:
- राज्यपाल चुनाव के बाद सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं।
- मुख्यमंत्री के पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है।
- मंत्रिपरिषद की नियुक्ति:
- मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
- मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं और यह मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाना:
- राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
- कार्यकारी आदेश जारी करना:
- राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक मामलों को संचालित करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं।
- यह कार्य वे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।
- राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति:
- राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण करते हैं, आमतौर पर मुख्यमंत्री की सलाह पर।
- राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उपयोग:
- राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह कार्य वे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।
- राज्यपाल विभिन्न विभागों के सचिवों और अन्य उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं।
- राज्यपाल की सलाहकार समिति:
- राज्यपाल अपने परामर्श के लिए विभिन्न समितियाँ और आयोग गठित कर सकते हैं।
- ये समितियाँ राज्य के विभिन्न मामलों में राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करती हैं।
- महामहिम का प्रतिनिधित्व:
- राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
- वे राज्य के मामलों में केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का पालन सुनिश्चित करते हैं।
राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ उन्हें राज्य के प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देती हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग मुख्यतः मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यपाल के कार्य संविधान के अनुसार और लोकतांत्रिक ढंग से होते रहें।
विधायी शक्तियां
राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ राज्य के विधायी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ राज्यपाल की प्रमुख विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है:
- विधानसभा के सत्र बुलाना और स्थगित करना:
- राज्यपाल विधानसभा के सत्रों को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
- विधानसभा का सत्र कम से कम वर्ष में एक बार बुलाना आवश्यक है।
- विधेयकों को स्वीकृति देना:
- राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। वे विधेयक को निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:
- स्वीकृति देना: विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना देना।
- वापस भेजना: विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजना।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना: कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना, विशेषकर जब विधेयक संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो या केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हो।
- पुनः प्रस्तुति: यदि विधेयक वापस भेजे जाने के बाद विधानमंडल द्वारा पुनः पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, तो वे इसे स्वीकृति या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।
- राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। वे विधेयक को निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:
- वित्तीय विधेयकों पर सिफारिश:
- राज्य का कोई भी वित्तीय विधेयक (मनी बिल) राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही वित्तीय विधेयक पर विचार किया जा सकता है।
- आवश्यक अध्यादेश जारी करना:
- जब विधानसभा सत्र में नहीं होती, तब राज्यपाल आवश्यक मामलों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, जो विधानमंडल के अगले सत्र में प्रस्तुत करना होता है।
- अध्यादेश की अवधि अधिकतम छह सप्ताह होती है, जब विधानमंडल सत्र में होता है।
- विधान परिषद के लिए नामांकन:
- जहाँ विधान परिषद (उच्च सदन) है, राज्यपाल उसमें 1/6 सदस्य नामित कर सकते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले होते हैं।
- जहाँ विधान परिषद (उच्च सदन) है, राज्यपाल उसमें 1/6 सदस्य नामित कर सकते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले होते हैं।
- सदस्यों को शपथ दिलाना:
- राज्यपाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
- राज्यपाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
- विशेष संबोधन:
- राज्यपाल हर वर्ष के पहले सत्र और राज्य के विधानसभा के प्रत्येक सत्र के पहले दिन विधानसभा को संबोधित करते हैं, जिसमें वे सरकार की नीतियों और योजनाओं का वर्णन करते हैं।
राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ राज्य के कानून निर्माण और विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, और ये शक्तियाँ राज्य के शासन और संविधान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
वित्तीय शक्तियाँ
राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ राज्य के वित्तीय मामलों के प्रबंधन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में राज्यपाल की प्रमुख वित्तीय शक्तियाँ विस्तार से बताई गई हैं:
- वार्षिक बजट प्रस्तुत करना:
- राज्यपाल राज्य का वार्षिक बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं।
- बजट में सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है और इसे विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है।
- वित्तीय विधेयक (मनी बिल):
- कोई भी वित्तीय विधेयक (मनी बिल) राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- मनी बिल पर चर्चा और पारित करने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है।
- वित्तीय आपातकाल की सिफारिश:
- राज्यपाल राज्य में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को वित्तीय आपातकाल (आर्थिक संकट) घोषित करने की सिफारिश कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है।
- राज्यपाल राज्य में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को वित्तीय आपातकाल (आर्थिक संकट) घोषित करने की सिफारिश कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है।
- वित्तीय खर्च की स्वीकृति:
- राज्यपाल बिना विधानमंडल की अनुमति के राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) से धन निकालने की स्वीकृति नहीं दे सकते।
- यदि आवश्यक हो, तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से आकस्मिक निधि (Contingency Fund) से धन निकालने की अनुमति दे सकते हैं, जिसे बाद में विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- अनुदान और अग्रिम राशि:
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान और अग्रिम राशि स्वीकृत कर सकते हैं।
- इन अनुदानों को बाद में विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- राजस्व वितरण:
- राज्यपाल राजस्व वितरण में अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करते हैं।
- यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी विभागों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय संसाधन मिलें।
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट:
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्टें राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा में प्रस्तुत की जाती हैं।
- ये रिपोर्टें राज्य के खातों और वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा के बाद तैयार की जाती हैं।
- वित्त आयोग की सिफारिशें:
- राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम करते हैं।
- राज्य वित्त आयोग राज्य के पंचायती राज संस्थानों और नगरपालिकाओं के लिए वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है।
राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ राज्य के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन शक्तियों का उपयोग राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ और सुचारू बनाने के लिए किया जाता है, ताकि राज्य की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
न्यायिक शक्तियाँ
राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ राज्य में न्यायिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में राज्यपाल की प्रमुख न्यायिक शक्तियाँ विस्तार से बताई गई हैं:
- दंड माफी (Pardon):
- राज्यपाल कुछ मामलों में दंड माफी, दंड कम करना, दंड स्थगित करना या दंड बदलने की शक्ति रखते हैं।
- यह शक्ति विशेष रूप से उन मामलों में होती है जिनमें राज्य के कानूनों के तहत सजा दी गई हो।
- मृत्युदंड माफी (Commutation of Death Sentence):
- राज्यपाल राज्य के न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड को माफ करने, बदलने या कम करने की शक्ति रखते हैं।
- हालांकि, यह शक्ति केवल राज्य के मामलों में लागू होती है और केंद्रीय कानूनों के तहत सजा पाए गए मामलों में यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
- दंड परिवर्तन (Commutation):
- राज्यपाल किसी अपराध के लिए दी गई सजा को एक कम कठोर सजा में बदल सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना।
- दंड स्थगन (Reprieve):
- राज्यपाल अस्थायी रूप से दंड स्थगित कर सकते हैं, जिससे दोषी व्यक्ति को कुछ समय के लिए दंड भुगतने से राहत मिलती है।
- यह स्थगन आमतौर पर किसी अन्य न्यायिक अपील या पुनर्विचार के लिए समय देने के उद्देश्य से किया जाता है।
- दंड निलंबन (Respite):
- राज्यपाल किसी विशेष परिस्थिति, जैसे गर्भावस्था या शारीरिक विकलांगता, के आधार पर दंड को निलंबित कर सकते हैं।
- यह अस्थायी राहत होती है और इसमें सजा की अवधि को कम नहीं किया जाता।
- दंड की शर्तों में बदलाव (Remission):
- राज्यपाल सजा की अवधि को बिना कानूनी तौर पर बदलते हुए कम कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, 10 साल की सजा को 5 साल में कम करना।
- विशेषाधिकार प्राप्त न्यायिक शक्ति:
- राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ विशेष परिस्थितियों में न्याय और मानवता के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए होती हैं।
- यह शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को प्रदान की गई हैं।
राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ राज्य के नागरिकों के प्रति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती हैं, जो न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। इन शक्तियों का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली की त्रुटियों को सुधारना और दया, मानवता, और न्याय को बढ़ावा देना है।
राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना
राज्यपाल की वीटो शक्ति का उपयोग विधायी प्रक्रियाओं में किया जाता है और इसका उद्देश्य किसी विधेयक को रोकना, संशोधित करना या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होता है। राज्यपाल की वीटो शक्तियों की तुलना राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं। निम्नलिखित में राज्यपाल की वीटो शक्तियों का विवरण और उनकी तुलना राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों से किया गया है:
राज्यपाल की वीटो शक्तियाँ:
- साधारण वीटो (Ordinary Veto):
- राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति देने से इंकार कर सकते हैं। इससे वह विधेयक अस्वीकार हो जाता है।
- यह शक्ति राज्यपाल का सबसे सामान्य वीटो होता है।
- सस्पेंसिव वीटो (Suspensive Veto):
- यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजते हैं और विधानसभा पुनः उसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर देती है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है।
- यह वीटो राज्यपाल को अस्थायी रूप से विधेयक को रोकने की शक्ति देता है।
- रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट (Reservation for the President):
- राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, विशेष रूप से यदि विधेयक संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करता हो या केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध हो।
- जेब वीटो (Pocket Veto):
- राज्यपाल किसी विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई कार्रवाई न करके उसे अप्रत्यक्ष रूप से रोक सकते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः कम किया जाता है।
राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ:
- साधारण वीटो (Ordinary Veto):
- राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति देने से इंकार कर सकते हैं। इससे वह विधेयक अस्वीकार हो जाता है।
- राष्ट्रपति की साधारण वीटो शक्ति भी व्यापक होती है।
- सस्पेंसिव वीटो (Suspensive Veto):
- राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं और यदि संसद पुनः उसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है।
- राष्ट्रपति का सस्पेंसिव वीटो संसद के संयुक्त सत्र द्वारा पारित विधेयकों पर लागू नहीं होता।
- जेब वीटो (Pocket Veto):
- राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई न करके उसे अप्रत्यक्ष रूप से रोक सकते हैं। जेब वीटो का कोई समय सीमा नहीं होती।
तुलना:
- साधारण वीटो: दोनों के पास साधारण वीटो की शक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि वे पूरे देश के विधेयकों पर वीटो का उपयोग करते हैं, जबकि राज्यपाल केवल अपने राज्य के विधेयकों पर।
- सस्पेंसिव वीटो: दोनों ही पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भेज सकते हैं, लेकिन पुनः पारित होने पर स्वीकृति देनी पड़ती है।
- जेब वीटो: राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास जेब वीटो की शक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति का जेब वीटो व्यापक रूप से जाना जाता है, जैसे राष्ट्रपति जिआनी जैल सिंह द्वारा 1986 में डाक विधेयक को रोकने के लिए इसका उपयोग।
- रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट: यह शक्ति केवल राज्यपाल के पास होती है और यह संविधान के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
राज्यपाल की वीटो शक्तियाँ राज्य के स्तर पर विधायी संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं, जबकि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक संतुलन और विधायी नियंत्रण को सुनिश्चित करती हैं।
अध्यादेश निर्माण में राज्यपाल के अधिकारों की शक्ति
राज्यपाल की वीटो शक्ति और अध्यादेश निर्माण में उनके अधिकार दोनों ही महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियाँ हैं, जो राज्यपाल को राज्य के विधायी और प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देती हैं। यहाँ इन दोनों शक्तियों का विवरण और तुलना दी गई है:
वीटो शक्ति:
- पूर्ण वीटो (Absolute Veto):
- राज्यपाल विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि विधेयक कानून नहीं बन पाएगा।
- इसका उपयोग सामान्यतः निजी सदस्य विधेयकों (Private Member Bills) पर किया जाता है।
- सस्पेंसिव वीटो (Suspensive Veto):
- राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं।
- यदि विधानमंडल विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से पारित करके राज्यपाल को भेजता है, तो राज्यपाल को विधेयक को स्वीकृति देनी होती है, सिवाय उन विधेयकों के जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- रिजर्वेशन वीटो (Reservation Veto):
- राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ऐसे विधेयक कानून नहीं बन सकते।
अध्यादेश निर्माण में राज्यपाल के अधिकार:
- अध्यादेश जारी करने का अधिकार:
- जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती, तब राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है।
- अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान होता है और यह तत्काल प्रभावी होता है।
- अध्यादेश की समय सीमा:
- अध्यादेश की वैधता अधिकतम छह सप्ताह की होती है जब विधानसभा पुनः सत्र में होती है।
- यदि इस अवधि में विधानमंडल द्वारा इसे पारित नहीं किया जाता, तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है।
- अध्यादेश जारी करने की शर्तें:
- राज्यपाल केवल तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- अध्यादेश मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किए जाते हैं।
- अध्यादेश का अनुमोदन:
- अध्यादेश जारी होने के बाद, इसे राज्य की विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- विधानसभा में इसे विधेयक के रूप में पारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा यह निरस्त हो जाता है।
वीटो शक्ति और अध्यादेश निर्माण की तुलना:
- अधिकार का उपयोग: वीटो शक्ति का उपयोग विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को नियंत्रित करने के लिए होता है, जबकि अध्यादेश निर्माण का अधिकार तब उपयोग किया जाता है जब विधानसभा सत्र में नहीं होती और तत्काल कानून की आवश्यकता होती है।
- नियंत्रण: वीटो शक्ति का उपयोग राज्यपाल के विवेकाधिकार पर आधारित होता है, लेकिन अध्यादेश निर्माण में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह महत्वपूर्ण होती है।
- समय सीमा: वीटो शक्ति का कोई विशेष समय सीमा नहीं होती, जबकि अध्यादेश की वैधता छह सप्ताह तक होती है जब विधानसभा पुनः सत्र में होती है।
- संवैधानिक नियंत्रण: दोनों शक्तियों का उपयोग संविधान के प्रावधानों के तहत किया जाता है, लेकिन अध्यादेश निर्माण में राज्यपाल की शक्तियाँ विधानमंडल द्वारा सीमित होती हैं, जबकि वीटो शक्ति अधिक स्वायत्त होती है।
इन दोनों शक्तियों के माध्यम से राज्यपाल राज्य की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कर्तव्य और अधिकार:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल के पद की स्थिति, कर्तव्य, अधिकार, और कर्मचारी विशेषाधिकारों को विस्तार से व्याख्या किया गया है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की समरी निम्नलिखित है:
- कर्तव्य और अधिकार:
- राज्यपाल का प्रमुख कर्तव्य राज्य के प्रशासन में समन्वय सुनिश्चित करना है।
- उन्हें राज्य के नियमन के लिए अधिकार होता है, जिसमें संविधान द्वारा प्रावधानित शक्तियाँ शामिल हैं, जैसे कि विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अभिमुख करने का अधिकार।
- राज्यपाल को विशेषाधिकार होते हैं, जिन्हें उन्हें संविधान और कानून द्वारा प्राप्त किया गया है। यह विशेषाधिकार राज्य की विशेष परिस्थितियों में उपयोग किए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 161 के तहत विशेषाधिकार:
- इस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में उपयोग किए जा सकते हैं। उनमें शामिल हैं:
- विधेयकों के पारित होने की प्रमाणित करने का अधिकार
- विधेयकों को राजपाल के पास भेजने का अधिकार
- उद्दीपन के अधिकार, यानी विधेयकों को रद्द करने या उन पर वीटो करने का अधिकार
- इस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में उपयोग किए जा सकते हैं। उनमें शामिल हैं:
- राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ:
- आपातकालीन स्थितियों में, जैसे कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा या विपदा के समय, राज्यपाल को विशेष प्राधिकार होते हैं।
- इन प्राधिकारों का उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में न्याय की व्यवस्था और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया जाता है।
- राज्यपाल की पदावधि:
- राज्यपाल की पदावधि पांच वर्ष होती है, लेकिन इसे राष्ट्रपति या राज्यसभा के पदस्थ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बढ़ाया जा सकता है।
- वह अपने पद की पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं।
इन सभी प्रावधानों के तहत, राज्यपाल को राज्य के प्रशासन में नेतृत्व और संवैधानिक स्थान का पालन करने की महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं।
राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में
राज्यपाल के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक कई प्रावधान हैं। ये अनुच्छेद राज्यपाल के कर्तव्य, अधिकार, और कार्यों को निर्धारित करते हैं। यहाँ उन अनुच्छेदों की संक्षिप्त सूची है:
- अनुच्छेद 153: राज्यपाल के पद का स्थापना और शपथ
- अनुच्छेद 154: राज्यपाल के कार्यक्षेत्र
- अनुच्छेद 155: राज्यपाल की पदावधि
- अनुच्छेद 156: राज्यपाल के नियुक्ति और शपथ
- अनुच्छेद 157: राज्यपाल के उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 158: राज्यपाल के अधिकार
- अनुच्छेद 159: राज्यपाल के कार्यों का विवरण
- अनुच्छेद 160: राज्यपाल के उपाधिकारियों का पद
- अनुच्छेद 161: राज्यपाल की विशेषाधिकार
- अनुच्छेद 162: राज्यपाल के नियुक्तियों की प्राधिकारिकता
- अनुच्छेद 163: राज्यपाल की विशेष शक्तियां
- अनुच्छेद 164: राज्यपाल के कार्यों के लिए ज़िम्मेदारी
- अनुच्छेद 165: राज्यपाल के पास विधेयकों की पुनर्विचार शक्ति
- अनुच्छेद 166: राज्यपाल के उपाध्यक्ष के रूप में पद का स्थानांतरण
- अनुच्छेद 167: राज्यपाल के राज्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में विशेष उपाध्याय