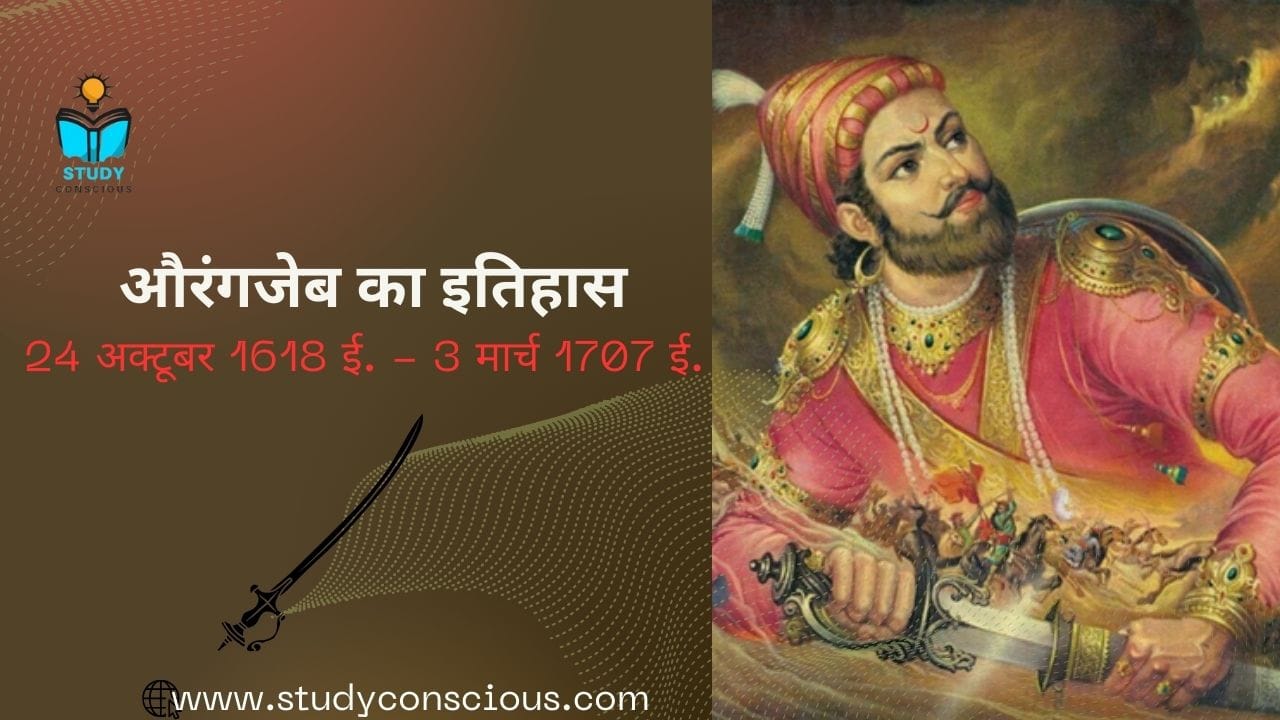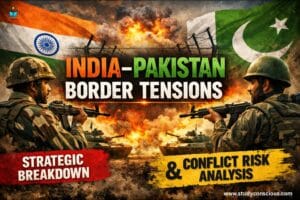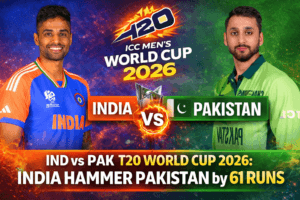औरंगज़ेब, जिनका पूरा नाम अबुल मुज़फ्फर मोहिउद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था, का जन्म 3 नवम्बर 1618 को गुजरात के दौलताबाद में हुआ था। वह मुग़ल साम्राज्य के छठे शासक थे और 1658 से 1707 तक शासन किया। औरंगज़ेब को उनके पिता शाहजहाँ ने 1636 में दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया था, जिससे उनकी प्रशासनिक और सैन्य कौशल का विकास हुआ।
जन्म – 24 अक्टूबर,1618 ई.
जन्म स्थान – दोहद (उज्जैन के पास)
पूरा नाम – मुहीउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब
माता – मुमताज महल
पिता- शाहजहाँ
उपाधि – बहादूर( शाहजहाँ द्वारा दिया गया)।
राज्यभिषेक – दो बार पहला – 21 जूलाई 1658 ई. दूसरा – 15 जून, 1659 ई.

प्रारंभिक जीवन और सत्ता में आना
औरंगज़ेब शाहजहाँ और मुमताज़ महल के पुत्र थे। उनके शासनकाल की शुरुआत काफी संघर्षमय रही। 1657 में जब शाहजहाँ बीमार पड़े, तब उनके चारों पुत्रों – दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श, और औरंगज़ेब – के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को पराजित कर सत्ता हासिल की और अपने पिता शाहजहाँ को आगरा किले में बंदी बना लिया।
शासनकाल
औरंगज़ेब का शासनकाल मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार का काल था। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार और नीतियाँ लागू कीं:
- धार्मिक नीतियाँ: औरंगज़ेब को उनकी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने जज़िया कर को पुनः लागू किया और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया। इसके बावजूद, उन्होंने कुछ हिंदू राजाओं के साथ गठबंधन भी किया।
- प्रशासनिक सुधार: औरंगज़ेब ने प्रशासनिक क्षेत्र में कई सुधार किए। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए और कई गैर-ज़रूरी खर्चों को कम किया।
- विस्तार और युद्ध: औरंगज़ेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार युद्ध किए। उन्होंने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों को हराया और मराठों के साथ लंबे संघर्ष में लगे रहे।
विरासत
औरंगज़ेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य तेजी से गिरावट की ओर बढ़ गया। औरंगज़ेब के कठोर धार्मिक नीतियों और निरंतर युद्धों के कारण साम्राज्य के कई हिस्सों में असंतोष फैल गया, जिससे उनके उत्तराधिकारियों के लिए शासन करना मुश्किल हो गया।
आलोचना और प्रशंसा
औरंगज़ेब के शासनकाल की आलोचना और प्रशंसा दोनों की जाती है। जहाँ एक ओर उन्हें धार्मिक कट्टरता और अत्याचार के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें उनके प्रशासनिक कौशल और साम्राज्य के विस्तार के लिए सराहा जाता है।
औरंगजेब के पुत्र
औरंगज़ेब के कई पुत्र थे, जिनमें से चार प्रमुख थे। इन चार पुत्रों का नाम मुहम्मद सुल्तान, मुअज्जम (जिसे बहादुर शाह I के नाम से भी जाना जाता है), मोहम्मद आजम शाह, और काम बख्श था। इन सभी का अपने पिता के शासनकाल और मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
1. मुहम्मद सुल्तान
मुहम्मद सुल्तान औरंगज़ेब का सबसे बड़ा पुत्र था। उसे कई प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं, लेकिन 1676 में उसे अपने पिता के आदेश पर कैद कर लिया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
2. मुअज्जम (बहादुर शाह I)
मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह I के नाम से भी जाना जाता है, औरंगज़ेब का दूसरा पुत्र था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1707 में मुग़ल साम्राज्य की गद्दी संभाली। बहादुर शाह I ने 1707 से 1712 तक शासन किया और उनके शासनकाल में साम्राज्य ने स्थिरता प्राप्त की, लेकिन उनके शासनकाल के बाद मुग़ल साम्राज्य की शक्ति घटने लगी।
3. मोहम्मद आजम शाह
मोहम्मद आजम शाह औरंगज़ेब का तीसरा पुत्र था। वह भी एक महत्वपूर्ण सैन्य नेता था और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने भी सत्ता के लिए संघर्ष किया। हालांकि, बहादुर शाह I ने उसे हराया और वह 20 जून 1707 को आगरा के निकट एक युद्ध में मारा गया।
4. काम बख्श
काम बख्श औरंगज़ेब का सबसे छोटा पुत्र था। उसने दक्षिण भारत में शासन किया और अपने भाइयों के साथ सत्ता के लिए संघर्ष किया। बहादुर शाह I के खिलाफ संघर्ष में, काम बख्श को पराजित किया गया और उसकी मृत्यु 1709 में हो गई।
अन्य संताने
औरंगज़ेब की अन्य संताने भी थीं, लेकिन वे मुग़ल साम्राज्य की राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं थीं जितनी उनके प्रमुख पुत्र। इन चारों पुत्रों ने मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी गतिविधियों ने साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित किया।
औरंगज़ेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष मुग़ल साम्राज्य की गिरावट का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इसने साम्राज्य को अंदरूनी संघर्षों में उलझा दिया और उसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति को कमजोर कर दिया।
औरंगज़ेब की सूबेदारी
1. दक्कन (दक्षिण भारत) की सूबेदारी
औरंगज़ेब की सबसे महत्वपूर्ण सूबेदारी दक्षिण भारत में थी। उन्होंने कई बार दक्षिण भारत में सूबेदार के रूप में कार्य किया, जिससे उन्हें प्रशासनिक और सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ।
दक्कन में औरंगज़ेब की सूबेदारी के प्रमुख बिंदु:
- 1636 में पहली नियुक्ति: औरंगज़ेब को 1636 में दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। उस समय उनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण में मुग़ल साम्राज्य के प्रभाव को बढ़ाना और वहाँ के विद्रोहों को दबाना था।
- सैन्य अभियानों का नेतृत्व: औरंगज़ेब ने अपनी सूबेदारी के दौरान कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर, और अन्य स्थानीय राज्यों के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियानों का संचालन किया।
- प्रशासनिक सुधार: औरंगज़ेब ने दक्कन में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने कर प्रणाली को अधिक संगठित किया और राजस्व संग्रह में सुधार किया।
2. गुजरात की सूबेदारी
औरंगज़ेब ने गुजरात के सूबेदार के रूप में भी कार्य किया, जहाँ उन्होंने प्रशासनिक और राजस्व सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया।
गुजरात में औरंगज़ेब की सूबेदारी के प्रमुख बिंदु:
- 1635-1636 में नियुक्ति: औरंगज़ेब को 1635 में गुजरात का सूबेदार बनाया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया और प्रांत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया।
- स्थानीय विद्रोहों का दमन: गुजरात में सूबेदार रहते हुए उन्होंने कई स्थानीय विद्रोहों का दमन किया और मुग़ल साम्राज्य की शक्ति को मजबूत किया।
3. मुल्तान और सिंध की सूबेदारी
औरंगज़ेब को मुल्तान और सिंध की सूबेदारी भी सौंपी गई थी। इन सूबेदारियों में उनके कार्यकाल ने उन्हें उत्तर-पश्चिमी भारत की राजनीति और सैन्य स्थितियों का गहरा अनुभव दिया।
मुल्तान और सिंध में औरंगज़ेब की सूबेदारी के प्रमुख बिंदु:
- 1648 में नियुक्ति: औरंगज़ेब को 1648 में मुल्तान और सिंध का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और राजस्व प्रणाली में सुधार किए।
- सैन्य अभियानों का नेतृत्व: मुल्तान और सिंध में अपने कार्यकाल के दौरान, औरंगज़ेब ने क्षेत्रीय विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया।
औरंगज़ेब की सूबेदारियों का प्रभाव
औरंगज़ेब की सूबेदारियों ने उन्हें एक कुशल शासक और सैन्य नेता के रूप में विकसित किया। इन अनुभवों ने उन्हें साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों की विविधतापूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। उनकी सूबेदारियों के दौरान किए गए सुधार और सैन्य अभियान उनके भविष्य के शासनकाल के लिए नींव बने।
औरंगज़ेब की सूबेदारियों ने मुग़ल साम्राज्य को दक्षिण और उत्तर-पश्चिमी भारत में विस्तार और स्थायित्व प्राप्त करने में मदद की। उनके प्रशासनिक सुधार और सैन्य कौशल ने उन्हें एक मजबूत और प्रभावी शासक बनाया, जिसने उन्हें मुग़ल साम्राज्य के सम्राट बनने के लिए तैयार किया।
राज्याभिषेक की पृष्ठभूमि
1657 में, शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिसके बाद उनके चारों पुत्रों – दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श, और औरंगज़ेब – के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। शाहजहाँ अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन अन्य भाइयों ने इस फैसले को चुनौती दी।
सत्ता संघर्ष और औरंगज़ेब की विजय
- दारा शिकोह से संघर्ष: औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को हराने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ीं। 1658 में, समरगढ़ की लड़ाई में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को निर्णायक रूप से पराजित किया।
- शाह शुजा और मुराद बख्श: शाह शुजा और मुराद बख्श को भी औरंगज़ेब ने पराजित किया। शाह शुजा बंगाल में हार गया और मुराद बख्श को कैद कर लिया गया।
- शाहजहाँ को बंदी बनाना: औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लिया, जिससे उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की।
राज्याभिषेक
औरंगज़ेब का राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को हुआ। उन्होंने ‘आलमगीर’ (विश्व विजेता) की उपाधि धारण की और अपने शासनकाल की शुरुआत की। राज्याभिषेक समारोह आगरा में आयोजित किया गया था, जिसमें उच्च अधिकारी, रईस, और सेनापति शामिल हुए थे।
राज्याभिषेक की प्रमुख घटनाएँ
- समारोह और संस्कार: राज्याभिषेक समारोह बहुत ही भव्य और विधिपूर्वक संपन्न हुआ। इसमें औरंगज़ेब को शाही ताज पहनाया गया और उन्हें आधिकारिक रूप से मुग़ल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया।
- नए शासन की घोषणा: राज्याभिषेक के बाद, औरंगज़ेब ने अपनी नीतियों और शासन के मुख्य उद्देश्यों की घोषणा की। उन्होंने न्याय, प्रशासनिक सुधार, और इस्लामी कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
- धार्मिक नीति: औरंगज़ेब ने इस अवसर पर अपने धार्मिक दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया। उन्होंने इस्लामी कानून (शरिया) के आधार पर शासन करने का संकल्प लिया और कई धार्मिक सुधार किए।
राज्याभिषेक का महत्व
औरंगज़ेब का राज्याभिषेक मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह न केवल सत्ता परिवर्तन का प्रतीक था, बल्कि औरंगज़ेब की कठोर धार्मिक नीतियों और विस्तारवादी अभियानों की शुरुआत भी थी। उनके राज्याभिषेक ने साम्राज्य की राजनीतिक दिशा और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया।
औरंगज़ेब के शासन की विशेषताएँ
- धार्मिक नीतियाँ: औरंगज़ेब ने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित शासन की नींव रखी। उन्होंने जज़िया कर को पुनः लागू किया और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया।
- सैन्य अभियान: औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण भारत के बीजापुर और गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया और मराठों के साथ लंबा संघर्ष किया।
- प्रशासनिक सुधार: औरंगज़ेब ने प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और राजस्व संग्रह प्रणाली को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया।
औरंगज़ेब का राज्याभिषेक मुग़ल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने साम्राज्य की राजनीति, धर्म और प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। उनका शासनकाल मुग़ल साम्राज्य की शक्ति और सीमाओं दोनों का प्रतीक बन गया।
प्रारम्भिक कार्य
औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जो उनके प्रशासनिक कौशल, धार्मिक दृष्टिकोण और साम्राज्य को मजबूत करने के उनके इरादों को दर्शाते हैं। यहाँ उनके प्रारंभिक कार्यों के कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:
1. प्रशासनिक सुधार
अ. भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम: औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल की शुरुआत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उन्होंने उच्च पदों पर योग्य और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की और अनियमितताओं को सख्ती से दंडित किया।
ब. राजस्व सुधार: औरंगज़ेब ने राजस्व संग्रह प्रणाली में सुधार किए। उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित किया और किसानों से उचित कर संग्रह को सुनिश्चित किया।
2. धार्मिक नीतियाँ
अ. इस्लामी कानून (शरिया) का कार्यान्वयन: औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल की शुरुआत में इस्लामी कानून (शरिया) को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने न्यायपालिका और प्रशासनिक निर्णयों में शरिया का पालन सुनिश्चित किया।
ब. जज़िया कर का पुनः लागू होना: औरंगज़ेब ने 1679 में गैर-मुस्लिमों पर जज़िया कर पुनः लागू किया। यह कर हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम प्रजा पर लगाया गया था और यह औरंगज़ेब की धार्मिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
3. धार्मिक सहिष्णुता और कट्टरता
अ. मंदिर विध्वंस: औरंगज़ेब ने अपने प्रारंभिक कार्यों में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। यह कदम उनकी धार्मिक नीतियों के प्रति कट्टरता को दर्शाता है।
ब. इस्लामी संस्थानों का समर्थन: औरंगज़ेब ने मस्जिदों और मदरसों के निर्माण को प्रोत्साहित किया और धार्मिक विद्वानों और मौलवियों को आर्थिक सहायता प्रदान की।
4. सैन्य अभियान
अ. दक्षिण भारत के खिलाफ अभियान: औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने इन राज्यों को मुग़ल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया।
ब. मराठों के खिलाफ संघर्ष: औरंगज़ेब ने मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाए। मराठों के साथ संघर्ष उनके शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता रही।
5. अर्थव्यवस्था और व्यापार
अ. व्यापारिक नीतियाँ: औरंगज़ेब ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई। उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों के साथ व्यापारिक संबंधों को नियंत्रित किया और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास किए।
ब. कर प्रणाली में सुधार: औरंगज़ेब ने कर प्रणाली को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया। उन्होंने करों के संग्रह में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुधार किए।
6. सामाजिक सुधार
अ. शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध: औरंगज़ेब ने शराब और नशीले पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने नैतिकता और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया।
ब. सार्वजनिक कार्य: औरंगज़ेब ने सड़कों, सरायों, और जल आपूर्ति प्रणालियों जैसे सार्वजनिक कार्यों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।
7. न्याय प्रणाली में सुधार
अ. न्यायपालिका का पुनर्गठन: औरंगज़ेब ने न्यायपालिका का पुनर्गठन किया और अदालतों में न्याय की तेज़ी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुधार किए।
ब. स्थानीय विवादों का समाधान: औरंगज़ेब ने स्थानीय विवादों के समाधान के लिए पंचायतों और स्थानीय अदालतों को अधिक सशक्त बनाया।
औरंगज़ेब के प्रारंभिक कार्य उनके शासन की दिशा और उनकी नीतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उनके सुधारों और नीतियों ने मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक, और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया और उनके शासनकाल के कई वर्षों तक इनका प्रभाव बना रहा।
औरंगज़ेब के शासनकाल में पुर्तगालियों के प्रति नीति
औरंगज़ेब के शासनकाल में पुर्तगालियों के प्रति नीति और उनके साथ संबंध विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 17वीं शताब्दी में, पुर्तगाली भारत में कई स्थानों पर अपने उपनिवेश और व्यापारिक चौकियाँ स्थापित कर चुके थे, जिसमें गोवा उनका प्रमुख केंद्र था। औरंगज़ेब का पुर्तगालियों के प्रति रवैया और नीति उनके व्यापारिक गतिविधियों और सामरिक महत्व के आधार पर निर्धारित की गई थी।
पुर्तगालियों के प्रति नीति
- व्यापारिक संबंधों का नियंत्रण: औरंगज़ेब ने पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे, लेकिन वह इन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। पुर्तगालियों का व्यापार विशेषकर पश्चिमी समुद्र तटों पर बहुत महत्वपूर्ण था, और मुग़ल साम्राज्य को इससे राजस्व मिलता था।
- गोवा पर नियंत्रण: गोवा पुर्तगालियों का एक प्रमुख केंद्र था। औरंगज़ेब ने गोवा पर नियंत्रण के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं ले सके। गोवा का रणनीतिक महत्व था और पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति को कमजोर करना औरंगज़ेब की रणनीति का हिस्सा था।
- सैन्य संघर्ष और संघर्ष विराम: औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान, मुग़ल और पुर्तगाली बलों के बीच सैन्य संघर्ष भी हुआ। हालांकि, औरंगज़ेब ने पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचने की कोशिश की और कई बार संघर्ष विराम की स्थिति भी बनी रही।
- धार्मिक मुद्दे: पुर्तगालियों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण के प्रयासों को औरंगज़ेब ने सख्ती से देखा। पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन मुग़ल प्रशासन के लिए चिंता का विषय था, और इस पर नियंत्रण रखने के प्रयास किए गए।
- संधि और व्यापारिक समझौते: औरंगज़ेब ने व्यापारिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों के साथ संधियाँ और समझौते भी किए। इन संधियों के माध्यम से वह पुर्तगालियों के व्यापार पर नियंत्रण और सीमित सहयोग सुनिश्चित करना चाहते थे।
- पश्चिमी समुद्री मार्गों का सुरक्षा: औरंगज़ेब ने पश्चिमी समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया, ताकि पुर्तगालियों के समुद्री रास्तों पर कब्ज़ा न हो सके और भारतीय व्यापारियों के हित सुरक्षित रहें।
निष्कर्ष
औरंगज़ेब की पुर्तगालियों के प्रति नीति जटिल और बहुआयामी थी। एक ओर, उन्होंने पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे, जबकि दूसरी ओर, उन्होंने उनके प्रभाव और शक्ति को सीमित करने के प्रयास किए। उनके शासनकाल के दौरान, पुर्तगालियों के साथ संबंधों में व्यापारिक, सैन्य, और धार्मिक मुद्दों का मिश्रण दिखाई देता है। औरंगज़ेब की रणनीति का मुख्य उद्देश्य मुग़ल साम्राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, साथ ही पश्चिमी समुद्र तटों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करना था
औरंगज़ेब का अंग्रेजों के प्रति नीति
औरंगज़ेब का अंग्रेजों के प्रति नीति उनके व्यापारिक, राजनीतिक, और सैन्य हितों के आधार पर विकसित हुई। अंग्रेज उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में अपने व्यापारिक उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। औरंगज़ेब के शासनकाल में, अंग्रेजों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे। यहाँ औरंगज़ेब की अंग्रेजों के प्रति नीति के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:
व्यापारिक संबंध
- व्यापारिक संधियाँ: औरंगज़ेब ने अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए कई संधियाँ कीं। उन्होंने अंग्रेजों को भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति दी, विशेष रूप से बंगाल और पश्चिमी भारत में।
- व्यापारिक नियंत्रण: हालांकि औरंगज़ेब ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी, उन्होंने इस पर सख्त नियंत्रण बनाए रखा। अंग्रेजों को मुग़ल साम्राज्य के कानूनों और नियमों का पालन करना पड़ता था और उन्हें मुग़ल अधिकारियों को कर और शुल्क देना पड़ता था।
सैन्य और राजनीतिक नीतियाँ
- मद्रास और बॉम्बे में गतिविधियाँ: अंग्रेजों ने मद्रास और बॉम्बे (अब मुंबई) में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। औरंगज़ेब ने इन केंद्रों पर नजर रखी और सुनिश्चित किया कि ये केंद्र मुग़ल साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती न दें।
- सूरत की घेराबंदी: 1664 में मराठा नेता शिवाजी द्वारा सूरत पर आक्रमण के बाद, अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी का प्रयास किया। औरंगज़ेब ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह उनके नियंत्रण के बिना किया जा रहा था।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति संदेह: औरंगज़ेब अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और उनके इरादों के प्रति हमेशा सतर्क रहे। उन्हें शक था कि अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्तियाँ बनने की कोशिश कर रहे थे।
प्रमुख घटनाएँ
- बंगाल में संघर्ष: बंगाल में अंग्रेजों और मुग़ल अधिकारियों के बीच कई बार तनाव और संघर्ष हुए। 1686 में, अंग्रेजों ने चटगाँव, हुगली और कासिमबाजार में संघर्ष शुरू कर दिया, जिसे ‘चाइल्ड्स वॉर’ के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष के बाद, अंग्रेजों को बंगाल से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगकर औरंगज़ेब से संधि की और व्यापार की अनुमति प्राप्त की।
- व्यापारिक विशेषाधिकार: अंग्रेजों ने कई बार औरंगज़ेब से व्यापारिक विशेषाधिकार मांगे, जिनमें करों में छूट और व्यापारिक स्वतंत्रता शामिल थी। औरंगज़ेब ने इन विशेषाधिकारों को सीमित रूप से मंजूरी दी और सुनिश्चित किया कि मुग़ल साम्राज्य की संप्रभुता बनी रहे।
- औरंगज़ेब का पत्राचार: औरंगज़ेब और अंग्रेज अधिकारियों के बीच पत्राचार हुआ, जिसमें उन्होंने व्यापारिक शर्तों और नियमों पर चर्चा की। इन पत्रों में औरंगज़ेब का रुख कठोर और सावधान था, जिससे पता चलता है कि वह अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति को लेकर सतर्क थे।
निष्कर्ष
औरंगज़ेब की अंग्रेजों के प्रति नीति संतुलित और सतर्क थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे, लेकिन उनके राजनीतिक और सैन्य इरादों पर नजर रखी। औरंगज़ेब ने यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों की गतिविधियाँ मुग़ल साम्राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती न दें। उनका दृष्टिकोण वास्तविकता और व्यवहारिकता पर आधारित था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के साथ व्यापारिक लाभों का आनंद लिया, लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया।
औरंगज़ेब की उत्तर-पश्चिमी नीति
औरंगज़ेब की उत्तर-पश्चिमी नीति ने मुग़ल साम्राज्य की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं और सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नीति अफगानिस्तान, पंजाब, और कश्मीर के क्षेत्रों में मुग़ल साम्राज्य के प्रभुत्व को बनाए रखने और बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की गई थी।
1. अफगानिस्तान
काबुल और कंधार:
- औरंगज़ेब के शासनकाल में अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र था। मुग़ल साम्राज्य के लिए काबुल और कंधार का नियंत्रण आवश्यक था, क्योंकि ये क्षेत्र भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार मार्गों के केंद्र में थे।
- कंधार पर नियंत्रण के लिए औरंगज़ेब ने कई बार संघर्ष किया। शाहजहाँ के शासनकाल में यह क्षेत्र सफ़वीदों (फारस) के नियंत्रण में आ गया था। औरंगज़ेब ने इसे वापस प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया, लेकिन इसे पूरी तरह से मुग़ल नियंत्रण में लाना मुश्किल साबित हुआ।
2. पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमा
सिखों के साथ संघर्ष:
- औरंगज़ेब का शासनकाल सिख गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के समय से जुड़ा था। सिख धर्म के प्रति उनकी नीति कठोर थी और कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई।
- गुरु तेग बहादुर की गिरफ़्तारी और फांसी (1675) ने सिख समुदाय को औरंगज़ेब के खिलाफ कर दिया। इसके बाद, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और मुग़ल सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया।
उत्तर-पश्चिमी सीमा की सुरक्षा:
- उत्तर-पश्चिमी सीमा पर पठानों और अन्य कबीलों के साथ संघर्ष होते रहे। औरंगज़ेब ने इन क्षेत्रों में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए सैन्य अभियानों का सहारा लिया।
- पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुग़ल सेना की उपस्थिति और स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ के माध्यम से औरंगज़ेब ने अपने नियंत्रण को मजबूत किया।
3. कश्मीर
कश्मीर का प्रशासन:
- कश्मीर का क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता था। औरंगज़ेब ने कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और वहाँ पर मुग़ल प्रशासन की प्रभावी स्थापना की।
- कश्मीर में औरंगज़ेब ने कई धार्मिक और प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने सूफी संतों और धार्मिक विद्वानों को संरक्षण दिया, लेकिन साथ ही शिया मुस्लिमों पर सख्ती भी दिखाई।
4. बलूचिस्तान
बलूच कबीलों के साथ संबंध:
- बलूचिस्तान के क्षेत्र में बलूच कबीलों के साथ संघर्ष और समझौते होते रहे। औरंगज़ेब ने इन कबीलों को नियंत्रित करने और उनके साथ स्थिर संबंध बनाने का प्रयास किया।
- उन्होंने बलूच सरदारों को मुग़ल प्रशासन में सम्मिलित किया और उन्हें जागीरें प्रदान कीं, ताकि वे मुग़ल साम्राज्य के प्रति वफादार रहें।
नीति की विशिष्टताएँ
- सैन्य अभियान: औरंगज़ेब ने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में कई सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों का उद्देश्य मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और विद्रोहियों का दमन था।
- राजनयिक संबंध: औरंगज़ेब ने उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित विभिन्न कबीलों और शासकों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने गठबंधनों और संधियों के माध्यम से इन क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया।
- धार्मिक नीति: औरंगज़ेब की धार्मिक नीति कठोर और सख्त थी, विशेषकर सिखों और शिया मुसलमानों के प्रति। उन्होंने सुन्नी इस्लाम के सिद्धांतों का पालन किया और इसे अपने शासन का आधार बनाया।
- प्रशासनिक सुधार: औरंगज़ेब ने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने कर संग्रह, न्याय व्यवस्था, और स्थानीय प्रशासन को संगठित और प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए।
निष्कर्ष
औरंगज़ेब की उत्तर-पश्चिमी नीति ने मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, और धार्मिक कठोरता के माध्यम से इन क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया। हालांकि, उनके कठोर धार्मिक नीतियों और निरंतर सैन्य अभियानों ने कई बार स्थानीय असंतोष और विद्रोह को भी जन्म दिया। औरंगज़ेब की यह नीति उनके व्यापक प्रशासनिक और सामरिक दृष्टिकोण का हिस्सा थी, जिसने मुग़ल साम्राज्य की शक्ति और सीमाओं को प्रभावित किया।
औरंगज़ेब दक्षिण नीति
औरंगज़ेब की दक्षिण नीति मुग़ल साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों के प्रशासन और सुरक्षा को संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने पर केंद्रित थी। औरंगज़ेब के शासनकाल में दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में अधिकार, नियंत्रण, और न्याय की प्रवृत्ति रही। निम्नलिखित कुछ प्रमुख तत्व हैं जो औरंगज़ेब की दक्षिण नीति का हिस्सा थे:
1. राजनीतिक संबंध
निरंतर नियंत्रण:
- औरंगज़ेब के शासनकाल में दक्षिण भारत के राजनीतिक रूप को नियंत्रित रखने के लिए मुग़ल प्रशासन के विशेष ध्यान की आवश्यकता थी।
- उन्होंने दक्षिण भारत के राजा और नवाबों को नियंत्रण में रखा और उन्हें मुग़ल साम्राज्य की सामरिक सहायता के लिए आह्वान किया।
नवाबों का समर्थन:
- औरंगज़ेब ने दक्षिणी भारत के प्रमुख नवाबों का समर्थन किया ताकि वे स्थानीय शासन के अधिकार को बनाए रख सकें और मुग़ल साम्राज्य के साथ विश्वास का मान बनाए रखें।
2. सैन्य और सुरक्षा
सैन्य अभियान:
- औरंगज़ेब ने दक्षिणी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाए ताकि वहाँ के विद्रोहियों को दमन किया जा सके और सामरिक स्थिति को स्थायी बनाए रखा जा सके।
किले और गढ़ियों का निर्माण:
- औरंगज़ेब ने दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों पर किले और गढ़ियों का निर्माण करवाया ताकि वहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
3. धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियाँ
धार्मिक सुधार:
- औरंगज़ेब ने दक्षिणी भारत के धार्मिक संगठनों पर ध्यान दिया और सामाजिक सुधारों की प्रोत्साहना की।
- उन्होंने धार्मिक सहयोग और विरोध के माध्यम से सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास किया।
सांस्कृतिक प्रोत्साहन:
- औरंगज़ेब ने दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उत्थान का प्रोत्साहन किया। उन्होंने कला, साहित्य, और विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार की समीक्षा की और इन क्षेत्रों को ब
औरंगजेब और मराठे
औरंगजेब के शासनकाल में मराठा साम्राज्य के साथ संघर्ष और समझौता दोनों हुए। इस संघर्ष का कारण मुख्य रूप से भूमिगत और राजनीतिक कारणों से था।
संघर्ष
- करोंड़ा गणराज्य के विस्तार:
- मराठा साम्राज्य अपने प्रारंभिक दिनों से ही दक्षिण भारत में बढ़ता हुआ था। इसका विस्तार और शक्ति औरंगजेब के शासनकाल में हुआ।
- मराठों और मुग़लों के बीच भूमिगत संघर्ष बढ़ गया जब मराठा साम्राज्य अपने सत्ताधारिता का विस्तार करने के लिए मुग़ल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में हमला किया।
- कड़ा संघर्ष:
- औरंगजेब ने मराठों के प्रति कड़ा स्थित लिया। उन्होंने कई बार मराठों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए, लेकिन मराठे की गुटीयापन और जल्दबाजी के कारण उन्हें संघर्ष करने में समस्या हुई।
समझौता
- सांसदीय समझौता (1665):
- 1665 में, औरंगजेब ने मराठों के साथ सांसदीय समझौता किया। इस समझौते के तहत, मराठे और मुग़लों के बीच सीमा संबंधों का विवादित क्षेत्र निर्धारित किया गया और उन्हें उस क्षेत्र का कर वसूल करने का अधिकार दिया गया।
- अलाहाबाद समझौता (1666):
- इसके बाद, 1666 में, मराठों और मुग़लों के बीच अलाहाबाद समझौता हुआ, जिसमें मराठे ने मुग़ल साम्राज्य के साथ सांसदीय व्यापार को स्थायीता देने के लिए स्वीकार किया और उन्हें वर्तमान राज्य के लिए निर्धारित किए गए रक्षा अनुमोदनों के लिए भुगतान किया।
- सांसदीय तंत्र की स्थापना:
- यह समझौता सांसदीय तंत्र की स्थापना का पहला कदम था, जिसमें मराठे को राज्य की रक्षा के लिए मुग़ल साम्राज्य की सहायता की अनुमति मिली।
औरंगजेब की राजपूत नीति
औरंगजेब की राजपूत नीति उनके शासनकाल के दौरान विविध रही। उनके समय में राजपूत राजाओं के साथ संघर्ष और समझौता दोनों हुए। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे राजनीतिक, सामरिक, और आर्थिक।
संघर्ष
- केदारनाथ के युद्ध (1667):
- औरंगजेब ने केदारनाथ के युद्ध में मेवाड़ के राजपूत राजा राणा राजसिंह के खिलाफ सेना भेजी। इस युद्ध में मेवाड़ के राजा हारे और केदारनाथ किला मुग़लों के हाथों में आया।
- मारवाड़ के संघर्ष:
- औरंगजेब के समय में मारवाड़ के साथ संघर्ष भी हुआ। उन्होंने मारवाड़ के राजा राणा जयसिंह के खिलाफ युद्ध चलाया और 1679 में चितोड़ किले को जीता।
समझौते
- अम्बेर का समझौता (1669):
- 1669 में, औरंगजेब ने अम्बेर के राजा जयसिंह के साथ समझौता किया, जिसमें उन्होंने जयसिंह को अपने सेना में शामिल किया और उन्हें अमीर के रूप में स्वीकार किया।
- राजपूत राजाओं का अधिकार:
- औरंगजेब ने राजपूत राजाओं को उनके स्थानीय राज्यों में शासन करने का अधिकार दिया, जिससे उनका समर्थन और सहयोग प्राप्त हो सके।
- राजपूत सेना का समर्थन:
- औरंगजेब ने राजपूत सेना को भरोसा और समर्थन दिया, ताकि वे मुग़ल साम्राज्य के लिए सेना में शामिल हों और उनकी सेना को मजबूत करें
औरंगजेब की धार्मिक नीति
औरंगजेब की धार्मिक नीति विविधता और विवादों से भरी थी। उनके शासनकाल में धार्मिक प्रतिस्पर्धा, समझौता, और संघर्ष दोनों देखने को मिले।
धार्मिक संघर्ष
- हिन्दू धर्म के प्रति नीति:
- औरंगजेब के कुछ धार्मिक नियमों और नीतियों ने हिन्दू समुदाय के साथ विवाद पैदा किया। उन्होंने कुछ हिन्दू धर्मालम्बियों के स्थलों को तोड़ा और मस्जिद बनाई।
- जिज्या कर और धर्मनिरपेक्षता:
- औरंगजेब ने जिज्या कर को पुनः लागू किया, जिसमें गैर-मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता की दिशा में विशेष अधिकार मिले।
धार्मिक समझौते
- सिखों के साथ समझौता:
- औरंगजेब ने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता किया, जिसमें उन्होंने सिखों के स्थानीय अधिकारों को स्थायीता दी।
- हिन्दू धार्मिक नेताओं के साथ समझौता:
- कुछ हिन्दू धार्मिक नेताओं के साथ भी औरंगजेब ने समझौते किए, जिसमें उन्हें उनके स्थानीय धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में सहायता मिली।
धार्मिक साहित्य का प्रोत्साहन
- धार्मिक साहित्य का समर्थन:
- औरंगजेब ने धार्मिक साहित्य का प्रोत्साहन किया और उसे सामर्थ्यपूर्ण विद्यालयों में प्रवर्तित किया।
- धार्मिक वाद-विवाद का समर्थन:
- उन्होंने धार्मिक वाद-विवाद का समर्थन किया और उसे अधिकतम स्वतंत्रता और धार्मिक समझौता की दिशा में बढ़ावा दिया।
इस प्रकार, औरंगजेब की धार्मिक नीति उसके शासनकाल के दौरान विविधता और विवादों से भरी रही, जिसमें संघर्ष, समझौता, और सहयोग दोनों देखने को मिले।
औरंगजेब के समय में प्रमुख विद्रोह
औरंगजेब के समय में कई प्रमुख विद्रोह हुए जिनमें उनके शासनकाल की असमंजस्यपूर्णता और धार्मिक नीतियों के प्रति विरोध शामिल था। इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह निम्नलिखित थे:
- सतनामी विद्रोह (1672):
- सतनामी विद्रोह 1672 में उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह सिखों के धर्मगुरु गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के बाद हुआ था।
- जात विद्रोह (1672-1681):
- औरंगजेब के शासनकाल में मालवा, राजपुताना, और गुजरात क्षेत्र में जात समुदाय का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के दौरान, कई राजपूत राजाओं ने भी औरंगजेब के खिलाफ उठाव किया।
- जाट विद्रोह (1669):
- यह विद्रोह उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था जिसमें जाट समुदाय के सदस्यों ने औरंगजेब के नेतृत्व में बदलाव के खिलाफ उठाव किया।
- सिख विद्रोह (1688-1699):
- इस विद्रोह का मुख्य कारण था सिख धर्म के प्रमुख गुरु, गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का विरोध। इस विद्रोह के बाद, औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को पकड़वा के गहनों में बंधवाया और उन्हें मार दिया।
- राजपूत विद्रोह (1680-1707):
- औरंगजेब के शासनकाल में राजपूत राजाओं के बीच विवाद और विद्रोह हुए। इनमें मेवाड़, मारवाड़, अम्बेर, और जोधपुर शामिल थे।
औरंगजेब के समय महत्वपूर्ण घटना
औरंगजेब के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जो भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:
- बिजापुर, गोलकोंडा, और भोंला की जीत (1686-1687):
- औरंगजेब ने बिजापुर, गोलकोंडा, और भोंला के उत्तराधिकारियों को पराजित किया, जिससे वह दक्षिण भारत में अपनी सत्ता को मजबूत कर सके।
- सिख गुरु गोविंद सिंह के शहादत (1708):
- सिख गुरु गोविंद सिंह की शहादत और उनके औरंगजेब के बीच के संघर्ष ने सिख धर्म की भूमिका को मजबूत किया और सिखों के समुदाय को औरंगजेब के खिलाफ उत्तेजित किया।
- राजपूत विद्रोह (1680-1707):
- औरंगजेब के शासनकाल में राजपूत राजाओं के बीच विवाद और विद्रोह हुए, जो उनके राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया।
- काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण (1669-1675):
- औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को नष्ट करवाया और उनकी जगह पर मस्जिद बनवाई। यह घटनाएं धार्मिक सहमति और धार्मिक स्थलों के प्रति विवाद को बढ़ावा देने वाली थीं।
- मुघल साम्राज्य की वित्तीय संकट (1690-1707):
- औरंगजेब के शासनकाल में मुघल साम्राज्य का वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं था। उनकी वित्तीय संकट ने साम्राज्य की अस्थिरता को बढ़ाया और अंत में उनके शासनकाल का अंत हो गया।
औरंगजेब के मृत्यु –
औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। उनकी मृत्यु आगे के साम्राज्यिक और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दी, क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य में अनेक विवाद और संघर्ष हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद, मुघल साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो गई और वह संघर्षों से भरपूर साम्राज्यिक संकट का सामना करने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र मुआज़्ज़म और बहादुरशाह उनके परिवार के विवादों में अपने बहनों के साथ लड़ा। इससे मुघल साम्राज्य की लचीलापन और अस्थिरता और अधिक बढ़ गई।