सहकारी समितियां (Co-operative Societies) सामाजिक और आर्थिक संगठनों का एक प्रकार हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना होता है। ये संगठन स्वयंसेवी आधार पर स्थापित होते हैं और उनके सदस्य समान उद्देश्य और आवश्यकताओं के लिए एकत्रित होते हैं। सहकारी समितियों का प्रबंधन और संचालन उनके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, और प्रत्येक सदस्य को संगठन में समान अधिकार और जिम्मेदारी होती है।
- 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित तीन बदवालव किए:
- इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (धारा 19क)।
- सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य कके नीति-निदेशक सिद्धांत को जोड़ा (धारा 43 ख )।
- इसने संविधान में एक नया खंड IX – बी जोड़ा जिसका नाम ‘सहकारी समितियां (धारा 243 – ZH से 243- ZT) है।
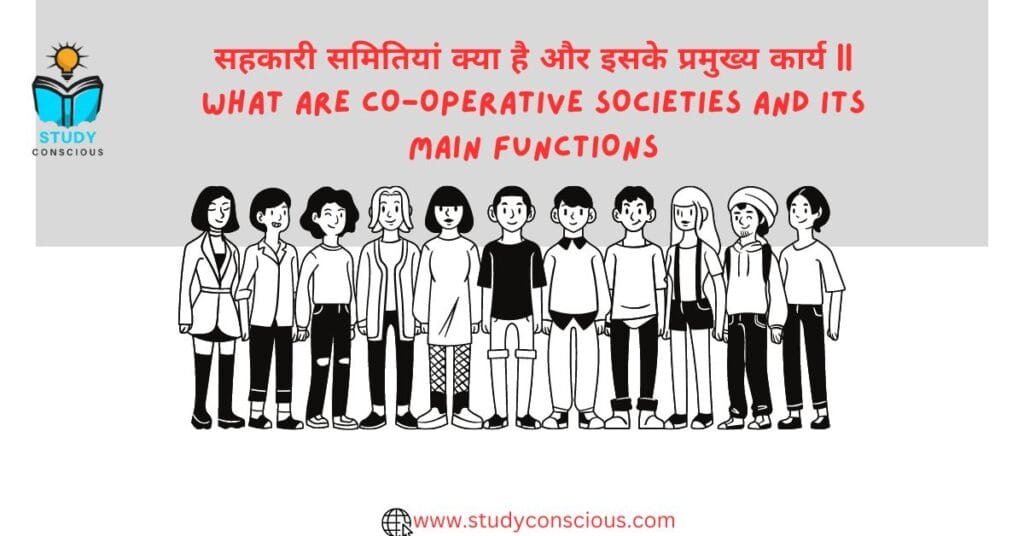
संवैधानिक प्रावधान
संविधान के खंड बी में सहकारी समितियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है:
सहकारी समितियों का संस्थापन: स्वैच्छिक गठन, सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता तथा स्वायŸा कार्यप्रणाली के सिद्धांतो के आधार पर राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संस्थान, नियम एवं बंद करने सम्बन्धी नियम बनाएगा।।
बोर्ड के सदस्यों एव इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें:
सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें आमतौर पर सहकारी समिति के प्रकार, आकार, और संबंधित कानूनों और नियमों पर निर्भर करती हैं। नीचे कुछ सामान्य शर्तें और नियम दिए गए हैं जो सहकारी समितियों में लागू होते हैं:
बोर्ड के सदस्यों की संख्या:
- संख्या: बोर्ड के सदस्यों की संख्या समिति की जरूरतों और आकार के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 5 से 21 सदस्यों के बीच होती है।
- निर्धारण: समिति की सामान्य सभा (General Body Meeting) में सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
पदाधिकारी:
बोर्ड के सदस्यों में से विभिन्न पदाधिकारी चुने जाते हैं, जो निम्नलिखित हो सकते हैं:
- अध्यक्ष (President/Chairperson):
- समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- समिति के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करता है।
- उपाध्यक्ष (Vice President/Vice Chairperson):
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है।
- सचिव (Secretary):
- समिति की बैठकों की सूचना देना और उनके कार्यवृत्त तैयार करना।
- सभी रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों का प्रबंधन करना।
- कोषाध्यक्ष (Treasurer):
- समिति के वित्तीय रिकॉर्ड्स का प्रबंधन करना।
- समिति के खातों का रखरखाव करना।
शर्तें और नियम:
- योग्यता:
- सदस्य को सहकारी समिति का सक्रिय सदस्य होना चाहिए।
- समिति के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक और समर्थन करने वाला होना चाहिए।
- चुनाव और अवधि:
- बोर्ड के सदस्यों का चुनाव आमतौर पर 3 से 5 साल की अवधि के लिए होता है।
- सदस्य पुनः चुनाव के लिए भी पात्र हो सकते हैं, यदि समिति के उपनियमों में ऐसा प्रावधान हो।
- नियमित बैठकें:
- बोर्ड की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें नीतियों, योजनाओं, और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- बैठक में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।
- त्यागपत्र और निष्कासन:
- कोई भी सदस्य स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
- किसी भी सदस्य को अनुशासनहीनता या समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर निष्कासित किया जा सकता है।
- अनुपस्थिति:
- यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसे बोर्ड से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी अनुपस्थिति को उचित कारणों से मान्य न किया गया हो।
- वेतन और भत्ते:
- बोर्ड के सदस्यों को आमतौर पर कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए भत्ता (allowance) दिया जा सकता है।
उपनियम और विनियम:
सहकारी समितियों के उपनियम (By-laws) और सरकारी नियमों (Regulations) में बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या और शर्तों के बारे में विस्तृत प्रावधान होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी बोर्ड सदस्य इन उपनियमों और विनियमों का पालन करें।
सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्य और पदाधिकारी समिति के सुचारु संचालन और लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका समर्पण और सामूहिक प्रयास समिति की सफलता में योगदान देता है।
सहकारी समितियों में बोर्ड के सदस्यों का चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया:
सहकारी समितियों में बोर्ड के सदस्यों का चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो समिति के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता और लोकतंत्र सुनिश्चित करती है। बोर्ड के सदस्य समिति के सर्वोच्च नीतिगत निर्णय लेने वाले होते हैं, इसलिए उनका चुनाव निष्पक्ष और सुसंगठित तरीके से होना आवश्यक है। चुनाव की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न होती है:
बोर्ड के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया:
- चुनाव की घोषणा:
- चुनाव की तारीख और स्थान की घोषणा समिति के नियमों के अनुसार की जाती है।
- सभी सदस्यों को चुनाव की जानकारी देने के लिए नोटिस भेजा जाता है।
- नॉमिनेशन (नामांकन):
- इच्छुक उम्मीदवार नामांकन पत्र भरते हैं और निर्धारित तिथि तक इसे जमा करते हैं।
- नामांकन पत्र में उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव, और समिति के प्रति प्रतिबद्धता की जानकारी दी जाती है।
- उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है और इसे सभी सदस्यों के लिए सार्वजनिक किया जाता है।
- जाँच और सत्यापन:
- नामांकन पत्रों की जाँच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- यदि कोई नामांकन अयोग्य पाया जाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है और संबंधित उम्मीदवार को सूचित किया जाता है।
- चुनाव प्रचार (Campaigning):
- पात्र उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने का समय और अवसर दिया जाता है।
- उम्मीदवार अपने विचार, नीतियाँ, और लक्ष्यों को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
- मतदान (Voting):
- मतदान का आयोजन निर्धारित तिथि और स्थान पर किया जाता है।
- मतदान गुप्त बैलेट (secret ballot) के माध्यम से किया जाता है ताकि सदस्यों के वोट गोपनीय रहें।
- प्रत्येक सदस्य को मतदान का अधिकार होता है और वे अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं।
- मतगणना (Counting of Votes):
- मतदान समाप्त होने के बाद, मतगणना की प्रक्रिया शुरू होती है।
- मतगणना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है, जिसमें उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति हो सकती है।
- परिणाम की घोषणा:
- मतगणना के बाद, चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं।
- विजयी उम्मीदवारों की सूची सभी सदस्यों को सूचित की जाती है।
- शपथ ग्रहण (Oath of Office):
- नव-निर्वाचित बोर्ड सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं और अपने पदों का कार्यभार संभालते हैं।
चुनाव प्रक्रिया की शर्तें और नियम:
- सदस्यता:
- केवल सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं।
- अवधि:
- बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल आमतौर पर 3 से 5 साल होता है, जो समिति के उपनियमों में निर्धारित होता है।
- निर्वाचन अधिकारी:
- एक स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
- अपील और विवाद:
- चुनाव परिणामों के खिलाफ किसी भी विवाद या आपत्ति की स्थिति में, एक अपील प्रक्रिया होती है जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है।
- पुनः चुनाव:
- बोर्ड के सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं यदि समिति के उपनियमों में ऐसा प्रावधान हो।
चुनाव प्रक्रिया का उद्देश्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है, जिससे सदस्य अपने प्रतिनिधियों को चुनकर समिति के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा सकें। यह प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता, और सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करती है, जो सहकारी समितियों के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है
बोर्ड का विघटन एवं निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन
सहकारी समितियों में बोर्ड का विघटन (dissolution) और निलंबन (suspension) अत्यंत गंभीर कदम होते हैं, जो असाधारण परिस्थितियों में उठाए जाते हैं। इसके साथ ही, ऐसी स्थिति में अंतरिम प्रबंधन (interim management) की व्यवस्था भी की जाती है ताकि समिति का संचालन बाधित न हो। नीचे इन प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:
बोर्ड का विघटन (Dissolution of the Board)
- कारण:
- वित्तीय अनियमितताएँ या भ्रष्टाचार
- समिति के उद्देश्यों और नियमों का उल्लंघन
- सदस्यों की शिकायतें और असंतोष
- समिति के कार्यों में गंभीर लापरवाही या कुप्रबंधन
- कानूनी आदेश
- प्रक्रिया:
- जाँच: विघटन के संभावित कारणों की जांच एक स्वतंत्र समिति या नियामक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।
- नोटिस: बोर्ड को विघटन का नोटिस दिया जाता है और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है।
- सुनवाई: बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में सुनवाई होती है जहाँ वे अपनी बात रख सकते हैं।
- निर्णय: अगर जाँच और सुनवाई के बाद बोर्ड को दोषी पाया जाता है, तो नियामक प्राधिकरण बोर्ड को भंग करने का आदेश जारी करता है।
बोर्ड का निलंबन (Suspension of the Board)
- कारण:
- तत्कालिक वित्तीय संकट
- सदस्यों की गंभीर शिकायतें
- अस्थायी अनुशासनहीनता
- बोर्ड के आंतरिक विवाद
- प्रक्रिया:
- जाँच: प्रारंभिक जांच की जाती है ताकि निलंबन के कारणों की पुष्टि की जा सके।
- नोटिस: बोर्ड को निलंबन का नोटिस दिया जाता है और उनकी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है।
- अस्थायी निलंबन: जांच पूरी होने तक बोर्ड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।
- सुनवाई और निर्णय: सुनवाई के बाद, यदि आवश्यक हो, तो निलंबन को स्थायी कर दिया जाता है या बोर्ड को बहाल कर दिया जाता है।
अंतरिम प्रबंधन (Interim Management)
- अंतरिम बोर्ड की नियुक्ति:
- जब बोर्ड भंग या निलंबित किया जाता है, तो एक अंतरिम बोर्ड या प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है।
- अंतरिम प्रबंधन के लिए सक्षम और अनुभवशील व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो समिति के कार्यों को संभाल सकें।
- कार्यक्षेत्र:
- अंतरिम प्रबंधन समिति के दैनिक कार्यों का संचालन करता है।
- वे वित्तीय रिकॉर्ड्स, संपत्ति, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रबंधन करते हैं।
- सदस्यता के मुद्दों और शिकायतों का निपटारा करते हैं।
- स्थायी बोर्ड का चुनाव:
- अंतरिम प्रबंधन एक निश्चित अवधि के लिए कार्य करता है, आमतौर पर तब तक जब तक स्थायी बोर्ड का पुनः चुनाव नहीं हो जाता।
- नए चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जाती है और सदस्यों के लिए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाता है।
- चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, नए चुने गए बोर्ड को कार्यभार सौंप दिया जाता है।
- रिपोर्टिंग:
- अंतरिम प्रबंधन अपनी गतिविधियों और निर्णयों की रिपोर्ट नियामक प्राधिकरण और सदस्यों को प्रदान करता है।
- वे वित्तीय रिपोर्ट्स और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
कानूनी पहलू:
- सहकारी समितियों के कानून और उपनियमों में बोर्ड के विघटन, निलंबन, और अंतरिम प्रबंधन के लिए स्पष्ट प्रावधान होते हैं।
- इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकरण सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- समिति के सदस्यों को भी इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी और समझ होनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही से पालन कर सकें।
बोर्ड का विघटन, निलंबन, और अंतरिम प्रबंधन सहकारी समितियों के सुचारु और पारदर्शी संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये उपाय समितियों की विश्वसनीयता और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं।
सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण (Audit of Cooperative Societies’ Accounts)
सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण (Audit of Cooperative Societies’ Accounts) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो समितियों की वित्तीय स्थिति और संचालन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। अंकेक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि समिति के वित्तीय लेनदेन सही तरीके से दर्ज किए गए हैं और नियमों के अनुसार किए गए हैं। नीचे सहकारी समितियों के खातों के अंकेक्षण की प्रक्रिया, महत्व, और आवश्यक प्रावधानों का विवरण दिया गया है:
अंकेक्षण की प्रक्रिया:
- अंकेक्षक की नियुक्ति (Appointment of Auditor):
- सहकारी समितियों के कानून और उपनियमों के अनुसार अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है।
- अंकेक्षक एक योग्य और मान्यता प्राप्त पेशेवर होता है, जिसे समिति की सामान्य सभा द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- कभी-कभी, सरकारी या नियामक प्राधिकरण भी अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं।
- वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा (Review of Financial Records):
- अंकेक्षक समिति के सभी वित्तीय रिकॉर्ड, जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की समीक्षा करता है।
- अंकेक्षक खातों के लेन-देन और वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और सत्यता की जांच करता है।
- साक्षात्कार और जाँच (Interviews and Verification):
- अंकेक्षक समिति के प्रबंधकों, लेखाकारों, और अन्य संबंधित व्यक्तियों के साक्षात्कार लेता है।
- समिति के विभिन्न वित्तीय लेन-देन और प्रक्रियाओं का निरीक्षण और सत्यापन करता है।
- भौतिक निरीक्षण (Physical Verification):
- समिति की संपत्तियों, नकदी, स्टॉक, और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की भौतिक जाँच की जाती है।
- अंकेक्षक यह सुनिश्चित करता है कि समिति की संपत्तियाँ और संसाधन सही तरीके से प्रबंधित हो रहे हैं।
- समेकन और विश्लेषण (Consolidation and Analysis):
- सभी डेटा और जानकारी को समेकित और विश्लेषण किया जाता है।
- वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की जाती है और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
- रिपोर्ट की तैयारी (Preparation of Audit Report):
- अंकेक्षक एक विस्तृत अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें सभी निष्कर्ष, टिप्पणियाँ, और सुझाव शामिल होते हैं।
- रिपोर्ट में समिति के वित्तीय स्थिति, लेन-देन की वैधता, और संचालन की कुशलता के बारे में जानकारी होती है।
- प्रस्तुति और समीक्षा (Presentation and Review):
- अंकेक्षण रिपोर्ट को समिति की सामान्य सभा और नियामक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- अंकेक्षक रिपोर्ट के निष्कर्षों और सुझावों की व्याख्या करता है और सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है।
अंकेक्षण का महत्व:
- वित्तीय पारदर्शिता (Financial Transparency):
- अंकेक्षण समिति के वित्तीय लेन-देन और संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- यह सदस्यों को यह विश्वास दिलाता है कि समिति का प्रबंधन ईमानदारी और कुशलता से किया जा रहा है।
- भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम (Prevention of Corruption and Fraud):
- अंकेक्षण संभावित वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, और धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने में मदद करता है।
- कानूनी अनुपालन (Legal Compliance):
- अंकेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि समिति के वित्तीय लेन-देन और संचालन सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन कर रहे हैं।
- प्रबंधकीय सुधार (Managerial Improvement):
- अंकेक्षक की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें समिति के प्रबंधन और संचालन को सुधारने में सहायक होती हैं।
- सदस्यों का विश्वास (Member Confidence):
- अंकेक्षण रिपोर्ट सदस्यों को समिति के वित्तीय स्वास्थ्य और संचालन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिससे उनका विश्वास बढ़ता है।
कानूनी प्रावधान:
- सहकारी समिति अधिनियम (Cooperative Societies Act):
- सहकारी समितियों के अंकेक्षण के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग अधिनियम और नियम बनाए गए हैं।
- इनमें अंकेक्षक की नियुक्ति, अंकेक्षण की प्रक्रिया, और रिपोर्टिंग के नियम शामिल होते हैं।
- नियामक दिशानिर्देश (Regulatory Guidelines):
- सहकारी समितियों के लिए नियामक प्राधिकरण (जैसे कि सहकारी विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है।
- ये दिशानिर्देश अंकेक्षण की गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।
निष्कर्ष:
सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण समिति के सुचारु संचालन, पारदर्शिता, और सदस्यों के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया समिति के वित्तीय स्थिति का सटीक आकलन प्रदान करती है और भविष्य के लिए सुधार के सुझाव देती है। अंकेक्षण के माध्यम से समिति के सदस्यों को यह सुनिश्चित होता है कि उनके हितों की रक्षा की जा रही है और समिति का प्रबंधन सही तरीके से किया जा रहा है।
97वें संशोधन के कारण
भारत में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के प्रबंधन और संचालन को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और कुशल बनाना था। यह संशोधन सहकारी समितियों के संविधानिक दर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, जिससे उनके प्रबंधन में सुधार हो और सदस्यों की भागीदारी बढ़ सके। 97वें संविधान संशोधन के प्रमुख कारण और प्रावधान निम्नलिखित हैं:
97वें संविधान संशोधन के प्रमुख कारण
- प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी:
- कई सहकारी समितियों में प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता की कमी थी। इससे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभाव:
- सहकारी समितियों में प्रायः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता था। समिति के सदस्यों की भागीदारी सीमित थी और प्रबंधन में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी।
- राजनीतिक हस्तक्षेप:
- कई सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उनके स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। इससे समितियों का उद्देश्य भटक रहा था।
- वित्तीय अस्थिरता:
- वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन के कारण कई सहकारी समितियां वित्तीय संकट में थीं। इससे सदस्यों का विश्वास कम हो रहा था और समितियों की विश्वसनीयता घट रही थी।
97वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान
- संविधान में समावेश:
- सहकारी समितियों को संविधान के भाग IX-B (संविधान के अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक) के तहत शामिल किया गया, जिससे उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- मूल अधिकारों की सुरक्षा:
- सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) के तहत शामिल किया गया, जिससे किसी भी व्यक्ति को सहकारी समिति बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार मिला।
- प्रबंधन में सुधार:
- सहकारी समितियों के प्रबंधन और संचालन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नियम बनाए गए।
- समितियों के चुनाव नियमित रूप से कराने और निर्वाचित सदस्यों की समय सीमा निर्धारित करने के प्रावधान किए गए।
- स्वतंत्रता और स्वायत्तता:
- सहकारी समितियों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए, जिससे बाहरी हस्तक्षेप कम हो सके।
- राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि समितियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो।
- वित्तीय प्रबंधन:
- सहकारी समितियों के वित्तीय प्रबंधन और अंकेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए गए।
- नियमित अंकेक्षण और वित्तीय पारदर्शिता के प्रावधान किए गए।
- सदस्यों की भागीदारी:
- सहकारी समितियों के संचालन में सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए।
- सदस्यों को समिति के कार्यों और निर्णयों में सक्रिय भागीदारी का अधिकार दिया गया।
97वें संविधान संशोधन का प्रभाव
- सहकारी समितियों की सुदृढ़ता:
- इस संशोधन के बाद सहकारी समितियों के प्रबंधन में सुधार हुआ और उनकी सुदृढ़ता बढ़ी।
- लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन:
- सहकारी समितियों में चुनाव प्रक्रिया अधिक नियमित और पारदर्शी हो गई, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित हुआ।
- वित्तीय पारदर्शिता:
- वित्तीय अंकेक्षण और प्रबंधन में सुधार के कारण समितियों की वित्तीय स्थिति बेहतर हुई।
- सदस्यों का विश्वास:
- सदस्यों की भागीदारी बढ़ने और प्रबंधन में सुधार के कारण सहकारी समितियों में सदस्यों का विश्वास बढ़ा।
97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक और स्वायत्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सहकारी आंदोलन को सशक्त किया और सहकारी समितियों के सदस्यों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की।
सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में
97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के लिए एक समर्पित खंड शामिल किया, जिसे भाग IX-B कहा जाता है। इस खंड में सहकारी समितियों के गठन, संचालन और प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद शामिल हैं। इन अनुच्छेदों का उद्देश्य सहकारी समितियों की स्वायत्तता, लोकतांत्रिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यहाँ पर सहकारी समितियों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है:
भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद (भाग IX-B)
- अनुच्छेद 243ZH: परिभाषाएँ (Definitions)
- इसमें सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं, जैसे “सहकारी समिति”, “सदस्य”, “राज्य सहकारी समिति अधिनियम”, आदि।
- अनुच्छेद 243ZI: सहकारी समितियों का अधिकार (Right to form Cooperative Societies)
- इस अनुच्छेद के तहत, नागरिकों को सहकारी समितियाँ बनाने और उनमें शामिल होने का अधिकार दिया गया है। यह एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है।
- अनुच्छेद 243ZJ: प्रबंधन का संचालन (Incorporation, regulation and winding up of cooperative societies)
- सहकारी समितियों के गठन, विनियमन, और समाप्ति के लिए राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसमें समितियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नियम और विनियम शामिल हैं।
- अनुच्छेद 243ZK: चुनाव (Election of members of board)
- इस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। चुनाव नियमित अंतराल पर, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने चाहिए।
- अनुच्छेद 243ZL: कार्यकाल और दायित्व (Term of office of elected members of board and its office bearers)
- इसमें निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों के कार्यकाल और उनके दायित्वों का विवरण शामिल है। आमतौर पर, कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
- अनुच्छेद 243ZM: आरक्षण (Reservation of seats)
- इसमें बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 243ZN: बैठकें (Meetings of board)
- बोर्ड की बैठकों की आवृत्ति और उनके संचालन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। बोर्ड की बैठकें नियमित अंतराल पर होनी चाहिए।
- अनुच्छेद 243ZO: कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of Chief Executive and other officers of cooperative societies)
- इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनके दायित्वों का विवरण शामिल है।
- अनुच्छेद 243ZP: लेखों का अंकेक्षण (Audit of accounts of cooperative societies)
- सहकारी समितियों के खातों का वार्षिक अंकेक्षण कराने का प्रावधान है। अंकेक्षण एक पंजीकृत अंकेक्षक या सहकारी समितियों के अंकेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 243ZQ: सभा का आम बैठक (General Body meetings)
- इसमें सहकारी समितियों की आम सभा की बैठकों के आयोजन और संचालन का विवरण है।
- अनुच्छेद 243ZR: अंतर-सहकारी विवादों का निपटारा (Settlement of disputes)
- इसमें सहकारी समितियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के प्रावधान शामिल हैं।
- अनुच्छेद 243ZS: सहकारी समितियों की पुनरीक्षण (Supervision and control of cooperative societies)
- इसमें सहकारी समितियों की गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के प्रावधान दिए गए हैं।
- अनुच्छेद 243ZT: पूर्ववर्ती कानूनों का प्रभाव (Application to multi-State cooperative societies)
- यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के लिए लागू पूर्ववर्ती कानूनों के प्रभाव के बारे में विवरण देता है।
निष्कर्ष
97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों को भारतीय संविधान के तहत एक विशेष दर्जा प्रदान किया। इससे सहकारी समितियों के प्रबंधन और संचालन में सुधार हुआ और उनकी स्वायत्तता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। इन अनुच्छेदों ने सहकारी आंदोलन को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया।
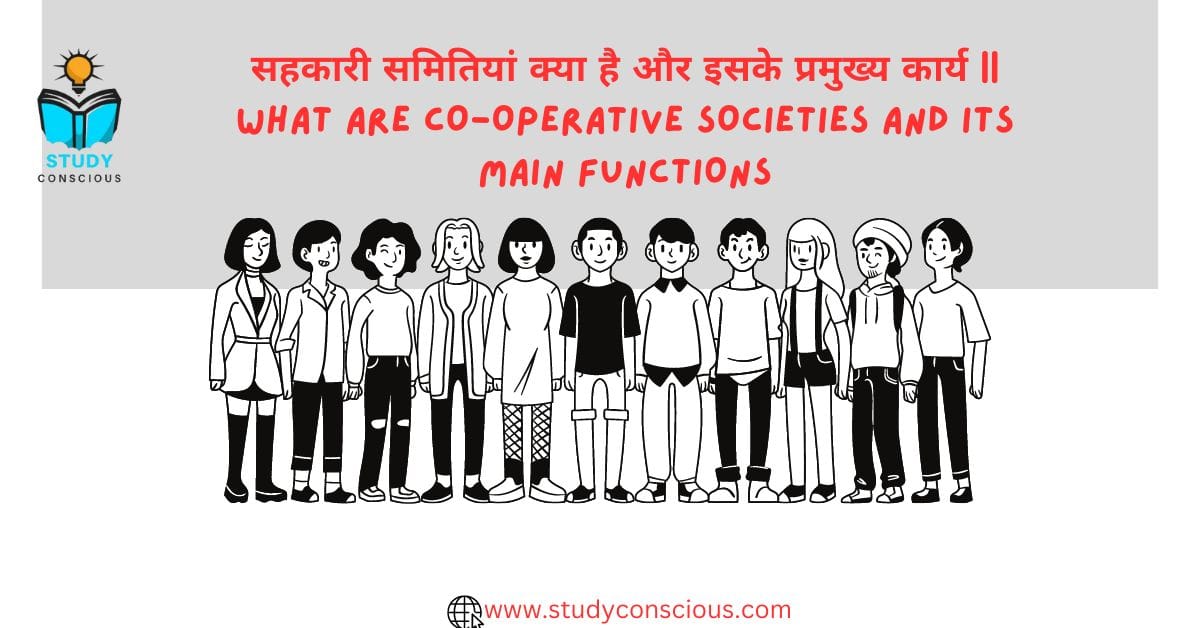



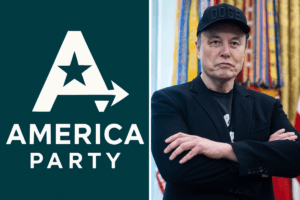

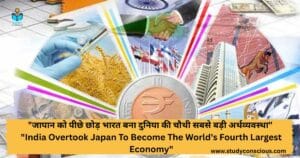





Nice……….Very good content
Hi Harsh! Thanks for the feedback, we really appreciate it.